
Call to Anytime
+91 9795550591
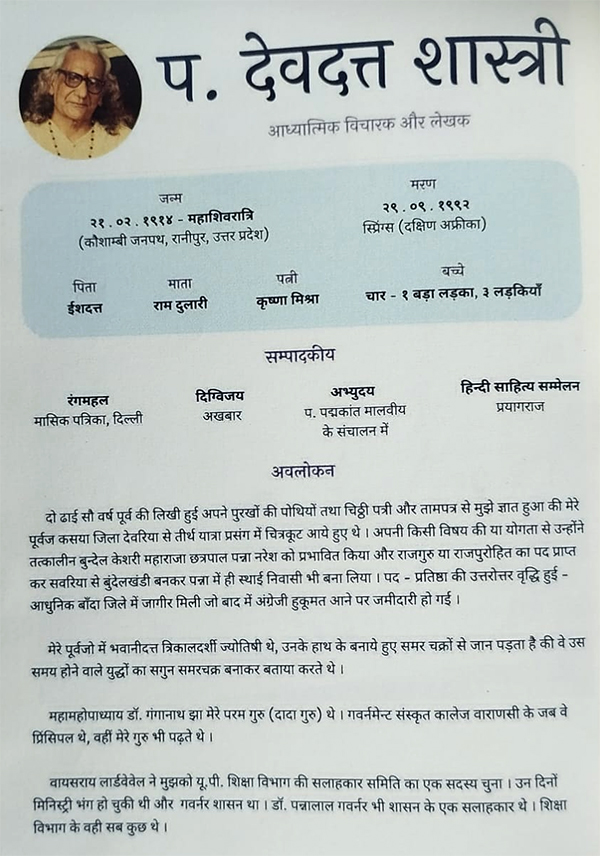
Pt Devdutt Shastri ji was born Mahashivratri 21 February 1914 in village- Ranipur, Pashchim Sharira (Janpath) of Kaushambi district (erstwhile Allahabad which is now Prayagraj) of Uttar Pradesh state of India. It is from Yajurvedi Brahmin and घृतकौशिक gotra and कुशहरा dynasty. Their ancestors were scholars and royal priests of the highest order, which they have clearly mentioned on the स्मृति के हस्ताक्षर. His father's name was Pt. Ishadutt Mishra who was a complete scholar of Jaiminya Samhita, Mimamsa and well-known ritualistic and mother's was Smt. Ramdulari Mishra, who was a gentle, serious and skilled housewife, being the youngest among all his brothers and sisters, he had a respect for Shastri ji. Mother's love was the highest.
Pt. Devdutt Shastri ji wrote about himself in his book "Bhuvaikunth Muktinath" as follows-
? Bakulam himself
There is a picture that has struck me. It always dominates me. All the time I have backache. It is not a picture of soil, stone, wood, paper or leaf, but a picture made of five elements, in which all the qualities and defects are inherent.
There are two sides to that picture -
Clean-shaded face with medium stature roundness, long nostrils looking for something - spectacles on eyes, dhoti-kurta on body, open head on which tangled - resolved, protruding, squinted hair.
Rural in speaking serious in appearance. Is he an atheist or a theist, a traditionalist or a progressive, a mystic or a realist, a sober or a pragmatist, a thinker or a translator. This is difficult to understand. Sometimes it writes in pure refined language and sometimes Ganga-Jamuni and sometimes by writing language, compels the reader to think that how much has been read, what has been read.
This aspect of the picture is multicolored. Sometimes it is tied in bonds, sometimes by breaking the turban, the bondage is freed. Sometimes extremely helpless in the punctuality of time, he lives every moment by being clever, agile and fit. Helpless in fulfilling the promise, hence careless in the eyes of the people. To understand whether he is a householder or a detached, greedy person or a renounced yogi is to understand that ghee is coming out with a straight finger.
The blueprint of his subconscious is visible in the other side of the picture. If someone could not be made a friend or a soulmate, then even an enemy was not allowed to arise. Very light and weak in digesting any thing either his own or foreign. To be so blunt that it is not an exaggeration to be called a dunce, but still there is no dearth of his affectionate relatives and well-wishers. Degree, without diploma, yet remained the editor-in-chief of high-end journals and sits among the scientists, sages. Acquainted with celebrities from every region of the country and abroad, also receives respect. Astonishingly, he is the author of eighteen subjects like mystery, history, science, sociology, political science etc. Writes and prints yet unliteral, burning. Nihang, wanderer, Yayavar.
A picture is formed by adding both the sides of the picture.
Whose noun is - "Devdatta"
Devadutt - a poor man. Poor parable of contradiction. For centuries, millennia, the burden of respect-disrespect, love-hate, prestige-disrespect has been carrying on both its shoulders. The sages, by performing the Vedic vowel process, made this nirukti, derivation and made Devadatta as Devashish. The commentators of Panini grammar, the Vartikakars expressed their love by presenting Devadatta as an example everywhere. In Mantras, Yantras and Tantras, Devadatta was made the target point. Later on, Buddhists tried to drink Devadatta by rubbing, grinding, rubbing, but he could not digest or even mouth. Then the Jataka tales got annoyed. I collected all the exceptions, stigmas, crimes, deceitfulness from all over the world and imposed them on Devadatta.
The blessings of the Vedic sect, the love-affection of the Vyakarana sect, the aim-bindu of the Agam sect and the insult of the Buddhist sect, these images with disrespect, have been ingrained in me since seventy two years. What is this picture of the impact of dialectical contradictions?
Brought up and nurtured by struggles. Tied by the chain of the principle ' even if broken, will not bow', a question mark of material life, firmly cherished faith and will power?
Similarly, Pandit Devdutt Shastri ji writes in his book "Smriti ke Hastakshar" - "From the books and letters of my ancestors written two and a half hundred years ago, I came to know that my ancestors had a pilgrimage from Kasaya district Deoria. Having come to Chitrakoot from Chitrakoot, he impressed the then Bundel Keshari Maharaja Chhatrapal Panna King with the merit of any of his subjects, and got the post of Rajguru and Rajpurohit and also made a permanent residence in Panna by becoming Bundelkhandi from Sanwaria. It grew progressively, got the jagir in the modern Banda district, which later became zamindari when the British came. Among my ancestors Bhavanidutt was a trikaldarshi astrologer, from his hand made samarchakro, it seems that the wars at that time were told by making Samarchakra. used to do."
Thus this scholar was naturally gifted due to his belonging to the lineage, his two brothers, the eldest being Pt Sridhar Mishra, who was a perfect master in Tantra Science, and the other Pt. Harihar Prasad Mishra who was a gold medalist in Ayurveda from the Lucknow Board.
Pandit Devdutt Shastri was educated in Rajapur Chitrakoot, and through self-study, he studied and learned Sanskrit, Hindi, English, science etc.
Mahamahopadhyay Dr. Ganganath Jha was his Paramguru i.e. Dadaguru.
In 1945, he was married to Krishna Mishra, born in a very rich and noble family, resident of Gohad village of Banda district, and they have a son Udayan and three daughters Bharti, Mallika & Sarika.
Pandit Devdutt Shastri made educational tours to many countries like Japan, Mauritius, Nepal, Korea, Zimbabwe, America, South Africa, Germany etc. and also received special honors from there.
Even today, his works are preserved for research in large libraries abroad, which can be seen on the website of world cat.
Pandit Devdutt Shastri was spared "Tajim" (special honour) by Maharana Udaipur and gifted a royal giant.
Viceroy Lordwell sent Pandit Devdutt Shastri to U.P. Elected member of the advisory committee of the Education Department.
Apart from this, Shastri ji also edited "Rangmahal" (Delhi monthly magazine), "Digvijay" (newspaper) and "Abhyudaya" magazine.
Along with this, he also worked as a high official in Hindi Sahitya Sammelan, Prayag. For some time, he also did teaching work in Dharmapadesh Sanskrit Mahavidyalaya, Malviya Nagar Prayagraj.
In 29 September 1992 Pandit Devdutt Shastri Ji transformed his body into Spring, South Africa through the yogic path of Padmasana.
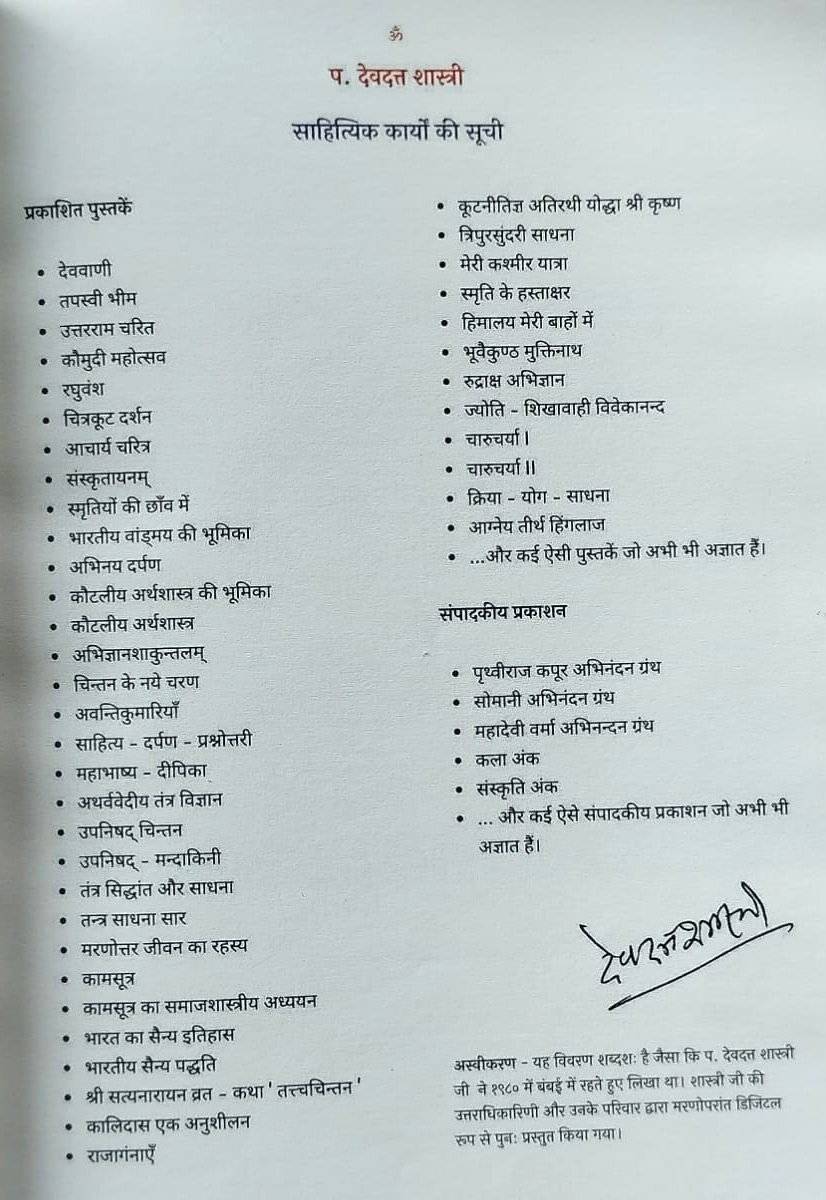
Apart from this, Pandit Devdutt Shastri wrote more than 200 books, which are still preserved in India and other countries, and he is known as the following Link-
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AS%CC%81a%CC%84stri%CC%84%2C+Devadatta%2C&fq&dblist=638&start=51&qt=page_number_link&fbclid=IwAR3s9rdxoS8kcJsWcCdoTfOdMdMmQil1DMXK2poKUi5wdbiLh3OrX7s37iQ#x0%253Abook-%2C%2528x0%253Abook%2Bx4%253Aprintbook%2529%2C%2528x0%253Abook%2Bx4%253Adigital%2529%2C%2528x0%253Abook%2Bx4%253Amic%2529formatMost of his books have The research has been done and there are still some things left which need to be researched.
Pandit Devdutt Shastri ji travelled all over India in the earlier part of his life, especially the entire Himalayas, which he mentioned in detail in "Himalaya Meri Baanho Mein". In the later part of his life, he was appointed as a linguist in Germany and then travelled to countries like England, America, Japan, Russia, Switzerland, Thailand, Australia etc. till the end of his life, and passed away while completing his last journey in South Africa. Some interesting incidents of his journey are given below-
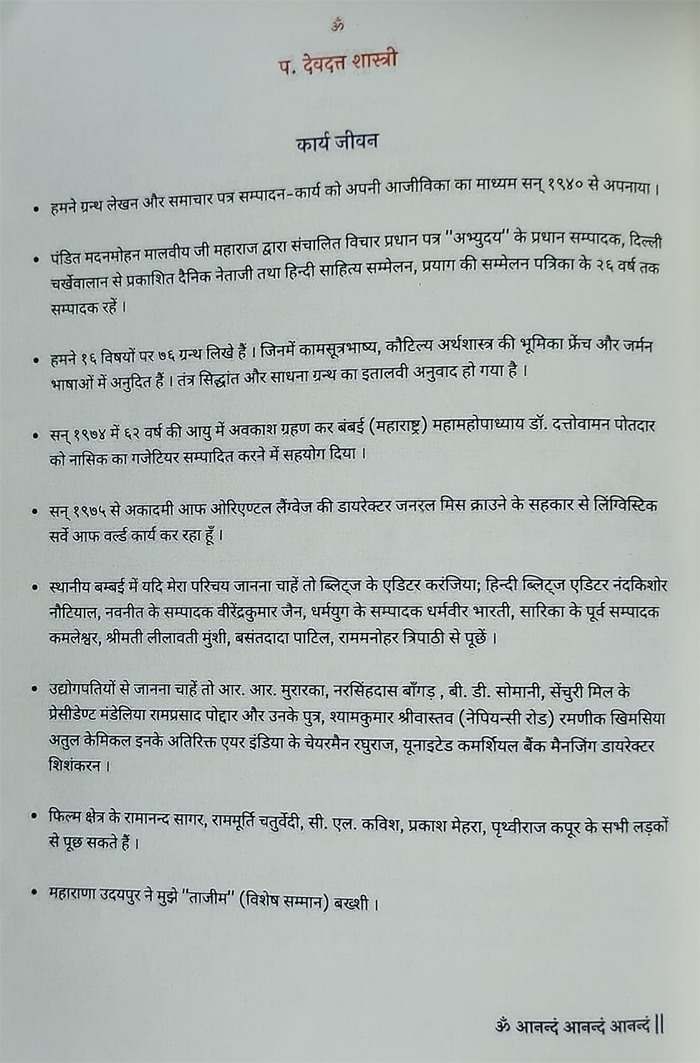
1)-कैलाश - मानसरोवर
भगवान् बदरीनाथ के प्रद्यान पुजारी श्री रावल का अथिति होकर मैं शान्तानन्द जी की प्रतीक्षा करता रहा । गन्धक के गर्म सोते में दिव्य स्नान करके भगवान् के दर्शन करता और फिर उन्ही का प्रसाद प्राप्त कर के बड़े आनन्द से प्रतीक्षा का समय बिता रहा था । शरीर पूर्ण स्वस्थ था । थकावट, क्लान्ति का कोई प्रभाव नहीं था । मन प्रसन्न और चित पुलकित था ।
एक दिन स्वामी शान्तानन्द जी आ पहुंचे । आते ही बोले -- स्वर्गारोहण हो आये क्षीरस्वामी !
क्षीरस्वामी -- यह नया संबोधन अपने लिए सुनकर मैं अचरज में पड़ गया । इधर - उधर देखने लगा कि शायद कोई संन्यासी - साधु और हो । शान्तानन्द जी समझ गए हुए हॅसते हुए बोले -- तुम्ही से पूछ रहे हैं, क्षीरस्वामी !
मैंने कहा -- स्वामी जी यह नया नाम कैसे रख दिया आपने ।
सतोपथ , स्वर्गारोहण कि यात्रा के बाद ।
आप से किसने बताया स्वर्गारोहण जाने कि बात ।
जिसके साथ सतोपथ से स्वर्गारोहण गए थे और फिर जो तुम्हे माणा तक पंहुचा आया था, उसी ने सब बताया । वह तुम्हे क्षीरस्वामी कहता था ।
लेकिन वह अरण्यमानव थो मुझसे बात ही नहीं करता था । वह मनुष्य था या देवता यक्ष, या प्रेत । वह थो अद्भुत जीव था स्वामी जी आपको कहाँ मिला था ।
कहीं भी मिला होगा, जाने दो । चलो तैयार हो जाओ जोशीमठ चल रहे हैं ।
हम बद्रिकाश्रम से २० मील दूर जोशीमठ दो दिन में आराम से पहुंचे । वहाँ तीन दिन बाद स्वामी शान्तानन्द बोले कैलाश - मानसरोवर के दर्शन करने के लिए कल चल देना हैं । स्वामी शान्तानन्द अनेक प्राच्यपाश्चात्य भाषाओं के विद्वान् होने के साथ ही उच्चकोटि की सिद्धियाँ प्राप्त किये हुए योगिनिष्ठ संत थे । हिमालय के अनेक परमसिद्ध सन्तों से उनका प्रत्यक्ष, परोक्ष संबंध था । उनमे ऐसी आध्यात्मिक शक्तियाँ थी कि जिस वस्तुकि इक्छा कि जाय उसकी सहजहि प्राप्ति हो जाती थी । इसलिए स्वामी जी के साथ चलने में तैयारी कि कोई खटर - पटर नहीं करनी पड़ती थी वह जब कहे, उसी समय मैं उनके साथ प्रस्थान केर देता था, किन्तु इस बार तो हिमालय - दर्शन का विशेष उदेश्य था सो कैलाश - मानसरोवर जाने के लिए आनाकानी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था । हिमायल कि पग - पग भूमि शान्तानन्दजी की नापी हुई थी । वह हर शृंग, शिखर, गिरिमला और नदी, स्रोत से परचित थे ।
जोशी मठ में ही शान्तानन्द जी ने परवतरोहण - अवरोहण की आवश्यक किन्तु संक्षिप्त साधन -सामग्री जुटा कर मुझे दे दी । दूसरे दिन होतीनीति घाटा होकर हम दोनों ने कैलाश - मानसरोवर के लिए प्रस्थान किया । जोशीमठ से सुरई ढोटा, मलारी, नीती, गुठिङ् होते हुए हम नीती घाट पहुँचे। गुठिङ् से नीतीघाट तक की चढ़ाई बड़ी प्राण लेवा थी । स्वामी जी के पास ऐसी जड़ी बूटियाँ और गुटिकाएं थी ; जिन्हें मुँह में रख लेने से ऊपर को चढ़ते हुए प्राण रुक जाते थे । बड़ी राहत मिलती थी । मक्खियों के काटने पैर घाव हो जाने पर बर्फीली हवाओं से देह फट जाने पर किसी वनस्पति की पत्तियाँ वे रगड़ देते थे, तो शरीर फिर से हरा - भरा हो जाता था । नीती घाट के बाद के पड़ावों के नाम तिब्बती होने के कारण मेरे स्मरण - पथ से दूर हो गए हैं । नीती - होती घाट से भारत के सीमा समाप्त होती थी, और तिब्बत की सीमा में प्रवेश किया जाता था । होती - नीती से रिमखिम तक उतराई बड़ी ही कठीन थी । स्वामी जी पर्वतीय मार्गो में चढ़ने, उतरने के अभ्यासी थे, किन्तु मेरे लिए तो तनिक सी चूक हो जाने पर जीवन का अस्तित्व ही मीट जाने का खतरा बना रहता था । दुर्गम पर्वत शिखरों पर चढ़ते, उतरते हम कैलाश पहुँचे थे ।
हिमालय के केदार खण्ड, बदरीखण्ड और कैलाश - मानखण्ड तीन भाग बताये जाते है । स्वामी जी ने बताया कि हम जिन पर्वतों, हिम - नादो, सरिताओं को पार करके आये हैं, वह सब कैलाश पर्वत श्रेणी के अन्तर्गत रहे हैं । तिब्बत भाषा में नदी को '' छू '' कहते हैं । शान्तानन्द जी ने बताया कि विस्तृत, वितत कैलाश खण्ड के अन्तर्गत '' ल्हाछू " और ' झोङ् छू ' इन दो नदियों से घिरा हुआ, जो पर्वत है, वही कैलाश है, कैलाश पर्वत के उत्तरी शीर्ष में शिवलिंग के आकर का शिखर है ।
हम लोग ग्रीष्म ऋतु में कैलाश पहुँचे थे । वहाँ हमें कई तिब्बती बौद्धलामा मिले थे, जो कैलाश की परिक्रमा के लिए आये हुए थे । हिन्दूधर्म और बौद्धधर्म में समानरूप से कैलाश - मानसरोवर की पूजा देवतीर्थ के रूप में की जाती है । कहा जाता है की कैलाश की एक परिक्रमा करने से एक जन्म के किये गए पाप नष्ट हो जाते है और दस परिक्रमाएँ करने से एक कल्प में किये गए पापों का क्षय हो जाता है । बौद्धलामा लोगों की धारणा है कि यदि कैलाश कि १०८ परिक्रमाएँ की जाएं तो सीधा निर्वाण प्राप्त होता है । वह मनुष्य आवागमन से रहित हो जाता है । जैसे हमारे यहाँ धनि लोग लोग गरीब ब्राह्मणों को भेजकर रामेश्वरम, पूरी आदि तीर्थों में जल चढ़वाते हैं, उसी प्रकार धनी तिब्बती लोग भी गरीब तिब्बतियों को भेड़े या रुपया देकर अपनी ओर से कैलाश - मानस यात्रएं कराकर पुण्ड अर्जित करते है । ऐसे तमाम लोग हमे कैलाश में मिले ।
हम लोग कैलाश की परिक्रमा का निश्चय कर चल पड़े । पाँच दिनों में पुरे कैलाश की परिक्रमा हमने पूरी की । कैलाश पर्वत के चारों ओर कई तिब्बती बौद्ध मठ हमें मिले । जैसे प्रयाग में अक्षयवट से कूद कर लोग मरा करते थे । यह विश्वास लेकर की सीधे वैकुण्ठ जायँगे । उसी तरह कैलाश परिक्रमा के अन्तर्गत चार स्थान ऐसे है, जिन पर तिब्बती भक्तों का यह विश्वास है कि वहाँ पर देह त्याग करने से निर्वाण मिलता है । इन स्थानों को तिब्बती भाषा में " थुतुप " कहते है । हमने मरते हुए तो किसी को नहीं देखा किन्तु अपना रक्त चढ़ाकर सर के केश चढ़ाकर लेटकर मरने का अभिनय करते हुए पचासों तिब्बतियों को हमने देखा है ।
जिस तरह कैलाश की परिक्रमा में चार थुटुप है, उसी प्रकार परिक्रमा के अन्तर्गत चार छक् छलगड् है । इन चारों स्थानों में लेटकर भक्तगण कैलाश की साष्टांग दण्डवत किया करते है । कैलाश पर्वत की दक्षिण तलहटी में तरछेन नाम का एक मठ है । यहीं से कैलाश परिक्रमा प्रारंभ की जाती है । कहा जाता है कि परिक्रमा की परिधि ३२ मील की है । परिक्रमा पथ पर डोलमा घाटी की चढ़ाई बड़ी भयानक है । लगभग १९००० फुट की ऊंचाई पर डोलमा स्थित है। इसी के पास पवित्र गौरीकुण्ड है । यहाँ बारहों महीने बर्फ जमी रहती है, लोग इसका पवित्र जल ले जाने के लिए बर्फ तोड़कर पानी निकालने का भगीरथ प्रयास किया करते हैं । कैलाश पर्वत के शिखर के नीचे १६००० फ़ीट की उचाई पर एक जड़ी बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती हैं, उसे कैलाश धुप कहते हैं । यह जड़ी बड़ी सुगंधित होती हैं और लता की तरह फैलती हैं । इसे सुखाकर हवन किया जाता हैं । कैलाश पर्वत की उत्तरी तलहटी में एक मठ के पा सफ़ेद रंग की मिट्टी मिलती हैं, उसे कैलाश भस्म कहते हैं, वह भस्म बड़ी पवित्र मानी जाती हैं I
मैं विश्व की बात तो नहीं कह सकता किन्तु मेरी द्दढ. धारणा हैं कि युग - युग से भारतीय जनता की आध्यात्मिक और धार्मिक भावना जाग्रत करने में प्रमुख हिमालय पर्वत और सर्वाधिक कैलाश पर्वत है। कैलाश साक्षात् प्राकृतिक शिवालय है । परमात्मा के रचना - कौशल का अद्भुत नमूना कैलाश है । मैंने कोहे काफ् से लेकर अलताई, लुशाई, पाटकोई पर्वत तक हिमालय का भ्रमण किया है । गौरीशंकर और सरगमाथा जैसे विश्व के सर्वोच्च पर्वतों को देखा है किन्तु कैलाश पर्वत के दर्शन कर मैं भावाभि भूत हो उठा । कैलाश को देखते ही बरबस मैं दण्डवत लेट गया । मुझे ऐसा लग रहा था कि पीछे से मेरे दोनों पैरों को खीच रहा है । अद्भुत सौन्दर्य, अद्भुत, आकर्षण और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति गिरिवर कैलाश में है । साक्षात् शिव रूप वही देखने को मिला । ऐसा स्पष्ट दिखता है कि एक विशाल पीठिका पर विराट शिव लिंग स्थापित है ।
यह राजताद्रि छण - छण में अपने सौन्दर्य में परिवर्तन करता हुआ - सा प्रतीत होता है । बारहों मास हिमाच्छादित रहने वाला यह देवतात्मा पर्वत नास्तिक से नास्तिक ह्रदय को भी श्रद्धा से अभिभूत कर प्रणिपात करा देता है हम हिन्दुओं के लिए धरती का यह स्वर्ग कैलाश स्फटिक स्वरुप है । इसके दर्शन मात्र से यह आभास होने लगता है कि इस रजत - आद्रि के शिखर पर शिव - पार्वती का नर्त्य हो रहा हो निः सन्देह मंगलमय भगवान् शिव तथा गिरिराज हिमायल कि पुत्री भगवती पार्वती की यह केलि - क्रिया भूमि है । यहाँ पर प्रकृती का पतिक्षण लास्य - नर्तन होता रहता है । कैलाश के चरणों के निकट पहुँचकर एक अनिवर्चिय - आनन्द की अनुभूति हुआ करती है ।
बाह्य - शक्ति - संपन्न स्वामी शान्तानन्द जी कैलाश शिखर पर स्थित शिव और पार्वती का साक्षात्कार कर समाधिस्थ हो गए थे । पुरे १० घंटे तक वह निर्विकल्प समाधि में निमग्नं थे, मैं भाव विभोर वहाँ बैठा रहा । कैलाश शिखर जगत की ऐश्वर्यमयी विभूति है, इसका सौन्दर्य वर्णनातीत है । उसकी स्वर्गीय छटा लिखने और पड़ने से नहीं प्रत्यक्ष दर्शन करने से ह्रदय के तार - तार, शरीर के रोम - रोम को पुलकित बना देती है । स्वेत, स्वच्छ हिम से आच्छादित कैलाश का शिखर शिव लिंग के समान प्रतिष्ठापित है ।शिवलिंग स्वरूप शिखर हिमपात होने से गोलाकार त्रिपुण्ड्र बन जाता है और उसके दक्षिण मुख में विशाल ऊध्वर्रपुण्ड्र बन जाता है । उस समय ऐसा विश्वास होता है कि सर्व शक्तिमान महाशिव की यह प्राकृतिक प्रतिमा है । यह दिव्य प्राकृतिक प्रतिमा प्रत्येक दर्शन में बलात श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न करती है । मैंने थो यहाँ तक अनुभव किया कि कैलाश के जाज्वल्यमाान रजत शिखर कि दिव्य छटा से समस्त हिमालय सुशोभित है । लगभग २३००० फुट कि ऊँचाई पर स्थित कैलाश पर्वत का उन्नत मस्तक नील - गगन को छेदता हुआ - सा जान पड़ता है । धरती और स्वर्ग दोनों को मिलाने वाला कैलाश पर्वत है ।
कैलाश के परिक्रमा - पथ से कुछ दूर मानसरोवर के रास्ते में एक बौद्धमठ में ल्हासा ( तिब्बत ) के ' टुलकू ' लामा क्रियाओं का अनुष्ठान कर रहे थे । स्वामी शान्तानन्द जी उनसे पूर्व परिचित थे । जब हम वहाँ पहुंचे तो टुलकूलामा ने शान्तानन्द जी कि ' ग्यगर लामागुरु ' कह कर सम्बोधित करते हुए उनका स्वागत किया । वह गुप्त क्रियाओं का अनुष्ठान कर रहे थे ऐसे अनुष्ठान एकान्त में किए जाते है, किसी दूसरे की दॄष्टि नहीं पड़ती है किन्तु टुलकू लामा ने पहले दिन ही शान्तानन्द जी को अपने अनुष्ठान कर्म में सम्मिलित कर लिया था । हम वहाँ पाँच दिन तक रहे । अन्तिम दिन टुलकूलामा ने मुझे बुलाकर मणिमंत्र की साधना की दीक्षा दी । अपने सान्निध्य में उन्होंने मुझे धारिणी,मुद्रा, ध्यानाभ्यास और आसन की विधि बताकर इष्टटदर्शन की प्रक्रिया बतलाई । मैं निहाल हो उठा । जब हम वहाँ से मानसरोवर के लिए चलने लगे तो उन्होंने मुझे पवित्र विभूति और कभी न मुरझाने वाली पुष्पमाला प्रदान की ।
स्वामी शान्तानन्द जी ने बहुत दिन बाद उनकी दिव्य शक्तियों का परिचय देते हुए बताया था कि टुलकू तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अवतारी महापुरुष । यह टुलकू लामा कई शताब्दियों से साधना रत है । अद्भुत तांत्रिक, यौगिक शक्तियाँ इन्हे प्राप्त है । किसी से कभी मिलते नहीं हैं । इनके जीवन काल में तीन दलाई लामा पीठसीन हुए हैं, किन्तु एक ने भी इनका साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया हैं । यह वीतराग, योगयुत्त महापुरुष हैं । हिमालय के विभिन्न स्थलों पर प्रकट, अप्रकट रूप से निवास किया करते हैं ।
कैलाश पर्वत से दक्षिण अनुमानत : बीस - पच्चीस मील पर पवित्र मानसरोवर और रावणह्रद ( राक्षस सरोवर ) अवस्थित है । राजहंसों, कलहंसों और विभिन्न प्रकार के पवित्र पक्षियों, महामत्स्यों, मत्स्यों से सुशोभित मानसरोवर विधाता की सष्टि की आदिम रचना है । जिस समय जल ही जल था, पृथ्वी बन रही थी या जल से निकल रही थी, उस समय मानसरोवर अपना भूगोल और इतिहास लिए स्तिथ था । यही पर सर्वप्रथम मानसी सष्टि हुई थी । दो सुविशाल रजतमय पर्वतों के मध्य गम्भीर शान्त भाव से यह पवित्र सरोवर अवस्थित है । जगमगाते हुए नीलमणि की भाँति इसका जल है । मानसरोवर के उत्तर में सर्वमङ्गलमय पवित्र श्री कैलाश है, दक्षिण में मान्धाता, पश्चिम में रावणह्रद ( राक्षस सरोवर ) और पूर्व में पर्वत श्रेणियाँ है । भूसर्वेक्षकों के मत से मानसरोवर समुद्र तल से १४९० फ़ीट ऊंचाई पर है । इसकी परिधि ५४ मील है । लम्बाई लगभग १७ मील और चौड़ाई लगभग १५ मील है ।
पवित्र मानसरोवर के चारों ओर सात - आठ बौद्धमठ है, जिसमें बौद्ध लामा निर्वाण प्राप्ति की कामना रखकर साधना - रत रहते है । चार चैत्य है, जो महासिद्धिलामाओं के स्मारक है ।
पुनीत मानसरोवर धरती में, मृत्युलोक में अवस्थित होते हुए भी अलौकिकता प्राप्त किये हुए भी अलौकिकता प्राप्त किये हुए है । देवता और मानव का, स्वर्गलोक और मृत्युलोक का मिलन पुनीत मानसरोवर में होता है । सरोवर की लोललहरें उसके वक्ष से उछल केर आकाश को सिंचित करती है । क्षण - क्षण भर में विभिन्न रूप धारण करता हुआ मानसरोवर प्रकृति नटी का क्रीड़ाक्रोड बना हुआ है । प्रातः काल सूर्योदय की रत्तिम स्वर्णिम किरणें जिस समय मानसरोवर के वक्ष पर पड़ती हैं, उस समय इंद्रधनुषी आकर धारण कर लहरें नर्तन करने लगती है । मध्याह्रकाल में उत्ताल तरंगे प्रतप्त सूर्यरश्मियों का सहारा लेकर स्फुलिंग बनकर समस्त वातावरण को प्रदीप्त कर देती हैं । अस्तंगत होते हुए सन्ध्या सूर्य की स्वर्णरश्मियाँ नील गगन और महोज्ज्वल नीलनीर मानसरोवर मिलकर चित्र विचित्र रंगों के वितान तानते हैं । अहर्निश मानसरोवर अपने सम्मोहन सौन्दर्य, अलौकिक शोभा से दर्शक और प्रकृति को सम्मोहित और विमुग्ध बनता है ।
हम जब मानसरोवर के तट पर पहुँचे थे, उस दिन आषाढ़ मास की गुरुपूर्णिमा थी । दो रजत शिखरों के मध्य महोज्ज्वल नील क्रान्ति मणि की भाँति स्थित मानसरोवर बिलकुल शान्त था । दिन का प्रथम प्रहर था । हमने जी भर कर स्नान किया । स्वामी शान्तानन्द तो हिमालयवासी ही थे । ३०० फुट गहरे सरोवर में प्रविष्ट होकर वह एक घण्टे तक डूबे हुए अधमर्षण मंत्र का जाप करते रहे । शीत, वात आतप के प्रभाव से परे शान्तानन्द एक महान योगी और परमसिद्ध सन्त थे । उन्होंने देह - सिद्धि प्राप्त कर ली थी । उन पर प्रकृति का, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था । और मैं तो इस क्षेत्र का आवारा रंगरूट था । मुझमें इतनी शक्ति,साधना कहाँ थी, कि मानसरोवर के आध्यात्मिक स्पन्दनों से अपने ह्रदय, मस्तिष्क, चेतना को आन्दोलित करता, फिर भी चाहे उस भूमि का प्रभाव हो, चाहे वातावरण का अथवा किसी अद्दश्य शक्ति का अनुग्रह हो, मुझे भी मानसराज के दिव्य सौन्दर्य, स्वर्गीय महत्त्व का कुछ न कुछ अनुभव हुआ । आनन्द की लहरें निरन्तर आध्यात्मिक स्पन्दन उछाल रही थी; लुटा रही थी; और मैंने भी आनन्द को यथाशक्ति लूटा ।
मानसरोवर में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य प्रतिदिन अनिर्वचनीय होते हैं, किन्तु हमारा यह सौभाग्य था कि उस दिन पूर्णिमा की ज्योत्सना भरी रात थी । आकाश नीरभ्र निर्मल था । मानस तट पर बैठे हुए हम जिस सुषमा का साक्षात्कार कर रहे थे, उसका वर्णन वाणी और लेखनी द्वारा संभव नहीं हैं । कोई चित्रकार या भावुक कवि भी उस अलौकिक सौन्दर्य को चित्रित या वर्णित करने में पूर्ण सफल नहीं हो सकता है ।
स्वामी शान्तानन्द तो पूर्णसमाधिस्थ थे और मैं आँखे खोले , कान खोले सरोवर के वछ से उठती हुई उत्तालतरंगो को देख रहा था । उनसे निकलती हुई स्पस्ट प्रणव - ध्वनि को सुन रहा था । कभी - कभी तो सरोवर महासागर - सा बनकर उत्तुंग तरंगो से प्रवण - नाद करता हुआ आकाश भेदन करने लगता था । कभी महाशिव लिंग बने कैलाश की स्पष्ट छाया उस पर दिखाई पड़ जाती थी और कभी चन्द्रमा और नक्षत्र - मंडल प्रतिबिम्बित हो उठते थे । मानसरोवर मानों एक पालना था, जिस पर कैलाश, मान्धता पर्वत और चन्द्रमा, नक्षत्रगण मुस्कुराते हुए झूल रहे है । कभी लहरें शान्त होकर मन्द-मन्थरगति से ऋचा - गान करती हुई - सी प्रतीत होती थीं । कुछ देर तक सरोवर निःशब्द, निःस्पंदन हो जाता और दूसरे छण महानाद करता हुआ अपनी तरंगों से आकाश को भर देता था ।
रात के तीसरे पहर अकस्मात् श्वेत सघन मेघ पुंजों से सारी धरती सारे पर्वत छिप गए । मानसरोवर एक श्वेत चमकती हुई लकीर - सा दिख रहा था । मैं घबरा उठा । मेरा आनन्द तिरोहित हो गया, इतने में शान्तानन्द जी तीन बार प्लुत स्वर से ओङ्कार उच्चारण कर अपनी समाधि भंग करते हुए बोले -- क्षीर स्वामी, आध्यात्मिक शक्तियाँ जलतरंगो में व्याप्त हो रही हैं । सावधान हो जाओ ? दिव्यता का ध्यान करो संकल्पनिष्ठ बनो ?
मैं सजग हो गया और फिर अनायास ध्यानस्थ हो गया । मुझे कुछ भी होश नहीं रहा । प्रातः सूर्योदय के समय मेरी चेतना लौटी । उस अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति कैसे प्रकट करू ? विवश हूँ । वह मेरे जीवन का सवर्प्रथम आध्यात्मिक स्पन्दन था ।
स्वामी शान्तानन्द की एक विचित्र प्रकृति थी । कभी वह मुझे घने जंगल, गिरी - द्रोणी या उपत्यका में छोड़कर चल दिया करते थे, यह कह कि जब तक वापस न आएँ यहीं रहना । कभी साल - साल भर लगा देते थे किन्तु मुझे विदा कर देते थे यह कह कर कि उचित समय पर मिलेंगे । इस बार तीन वर्ष बाद अचानक ऋषिकेश में मिले और बद्रिकाश्रम में मुझे छोड़कर एक महीने के लिए कहीं गुम हो गए । इससे मुझे अप्रत्याशित लाभ हुआ सतोपथ, स्वर्गारोहण के दर्शनों का । फिट कैलाश से मानसरोवर तक साथ रहे । एक बौद्ध मठ में मुझे ठहरा कर वह मानसरोवर पहुंचने के तीसरे दिन फिर गुम हो गए ।
मैं जिस मठ में ठहरा था, उसकी छत से भी कैलाश के दर्शन हुआ करते थे और उसी मठ से प्रकृति नटी कि भाँति प्रतिक्षण नया रंग - रूप धारण करने वाले मानसरोवर के दर्शन हुआ करते थे । मैं नित्य मानसरोवर स्नान करता था और घंटो उसी के चरणों में बैठकर अद्भुत, अनुपम अनिर्वचनीय आध्यात्मिक आनन्द का अनुभव किया करता था । मेरा ही नहीं जो भी मानसरोवर गए हैं, उन सब का यहीं कहना हैं, कि वहाँ पहुंच कर मन आक्षेप,विक्षेप रहित हो जाता हैं । ब्रह्म कि अनुभूति होती हैं । मनुष्य का चंचल मन तन्मय हो जाता हैं । कभी - कभी तो मानसरोवर ते तट पर ध्यानस्थ बैठकर मुग्धभाव से सारा दिन व्यतीत हो जाता था । कोई क्लान्ति नहीं, कोई विक्षेप नहीं पैदा होता था । कभी - कभी मैं लामाओं के साथ एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला जाया करता था । यात्री, लामा लोग मानसरोवर कि परिक्रमा किया करते हैं ।।।परिक्रमा करने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मील पाया किन्तु मैंने उसके सभी तटों के दर्शन अवश्य किए हैं ।
किसी तट पर बालुका - कण है, किसी पर कीचड है, किसी तट पर रत्नशीला खण्ड है और किसी किनारे पर विभूति मिलती है । कहीं - कहीं खिले हुए फूल और कहीं - कहीं रेशम से मुलायम घास और किसी जगह पर बिच्छू का - सा डंक मारने वाली घास है । कहीं पर मानस के किनारे पर पंख फड़फड़ाती हुई राज हंसों की पंक्ति सुशोभित है । कहीं पर उड़ - उड़कर राजहंस मानस के वक्ष पर विश्राम करते हैं । डुबकी लगाते हैं, तैरते हुए केलि - क्रीड़ा करते हैं । मानस की उत्तुंगतरंगो की टकराहट से मानसरोवर जो फेन उगलता है, वह फेन भी हंस की आकृति धारण कर लेता है, उस समय असली हंस और कृत्रिम फेनिलहंस को पहचानना मुश्किल हो जाता हैं ।
जिस मठ में मैं ठहरा था, वह दो मंजिला था । मठ के बाहर आँगन में मणिमंत्रलिखीत देवचित्रों से चित्रित, धर्म वाक्यों से अंकित एक धज्व लहरा रहा था । उसके आस - पास रंग - बिरंगी झण्डियाँ फहरा रही थी । मठ के अन्दर एक स्थान पर दश महाविद्यालयों में से प्रथम महाविद्या महाकाली और द्वितीय महाविद्या भगवती तारा की भव्य प्रतिमाएँ थीं । एक ओर अलोककेतेश्वर ओर उनकी शक्तियों की प्रतिमाएँ थीं, दूसरी ओर देवतत्व प्राप्त लामाओं ओर बुद्ध तथा बोधि सत्व की प्रतिमाएँ थीं । पूरा कमरा देवी - देवताओं से भरा हुआ था । मध्य में बौध्द लामा की साधना की स्थली एक स्थण्डिल पर थी । हर प्रतिमा के सामने मखन्न का दीपक जला करता था । एक अखंड दीपक बारहों महीने चौबीसों घण्टे जला करता था, जिसमें मन भर से अधिक मक्खन भरा रहता था । एक ओर धार्मिक हस्तलिखित पुस्तके रखी हुई थी । उनकी भी पूजा की जाती थी। प्रधान लामा के अतिरिक्त एक और लामा वहाँ रहते थे, जिन्हें पुजारी कह सकते हैं। वह नित्य सुबह शाम मानसरोवर में स्नान कर गन्ध, अक्षत, धुप, दीप, नैवैध से देव - परतिमाओं का पूजन किया करते थे । आषाढ़ी पूर्णिमा को उस मठ में विशेष समारोह से आराधना, पूजा हुई थी । कई लामा आकर जुट गए थे । रात में पंक्तिबद्ध होकर मोटे - मोटे आसनों पर बैठकर उन्होंने साधना की थी । पूजा के समय डमरू, शंख, शहनाई, तुरही, श्रृंगी, ढोल, मृदंग, व्रज, घंटी, घंटा, घड़ियाल आदि तरह - तरह के वाद्य बड़े लय - ताल से बजाए जाते थे ।
लामाओं की पूजा सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की थी । मनुष्यों की खोपड़ी, मध, मांस भी उनकी साधना, उपासना के अंग थे । टोंटीदार जलपात्र ( सागर ) में केसर मिश्रित जल भर कर देवताओं को स्नान कराया जाता था । स्थान - जल को चरणोदक के रूप में सब लोग पान किया करते थे ।
लामाओं की साधना, उपासना और आराधना में सर्वाधिक महत्त्व हवन को दिया जाता है । भिन्न - भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न - भिन्न हवन सामग्री और भिन्न प्रकार का हवनकुंड तथा प्रयोजन के अनुसार हवनमंत्र होते है । एक चौरस ( समचतुर्भुज ) कुंड मेरे रहते हुए हवन किया गया था, उस हवन का प्रयोजन विश्वशांति, अकाल, युद्ध - भय और पापों को दूर करने के लिए था । कुंड का नीचे का हिस्सा लाल रंग से, ऊपर का हिस्सा श्वेतरंग से रंगा था । कुंड के अन्दर पृथ्वी का ' लं ' बीज लिखा गया था । हवं सामग्री में कौन - कौन सी वस्तुएँ थी, किस काष्ठ की समिधा थी और कौन - कौन से मन्त्र थे, यह मैं नहीं समझ सका और न पूछ सका क्योंकि मैं तिब्बती भाषा जानता नहीं था । जितने दिन रहा संकेतो की भाषा से काम चलाता रहा ।
जिस मठ में मैं ठहरा हुआ था, उसका नाम ' चेरिकप गोम्पा ' था । तिब्बत्ती भाषा में मठ को गोम्पा कहते है । यहाँ तक पहुंचने में दाँतों पसीना आ गया था । बड़ी दुरस्त और निर्मम उतराई उतर कर इस गोम्पा में हम पहुंचे थे । गोम्पा के पास ही मानसरोवर के किनारे गुफाएँ बनी हुई है । उन गुफाओं में बौद्ध लामा रह कर साधना किया करते हैं । शीत, हिम से बचने के लिए ये गुफाएँ सुरक्षित स्थान है । मैं नित्य इन गुफाओं में साधना - रत लामाओं के पास जाया करता था । उनमें एक वयोवृद्ध ग्युट ( तंत्र शास्त्र ) के उच्च कोटि के विद्वान थे । मुझे बताया गया था कि उन वृद्ध लामा को अष्ट सिद्धियों में से चार सिद्धियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। शेष चार सिद्धियों के लिए साधनारत हैं । उनकी गुफा में रुद्राक्ष, काष्ठ, और सीसा, पारा कि बनी हुईं अनेक मालाएँ थी । हर माला में १०८ दाने थे। उन्होंने मुझे स्फटिक कि एक माला देकर अपने पास बैठकर कहा कि वज्रासन से बैठकर ओ ३ म् व्रज गुरु पद्म सिद्धि हुँ इस दशाक्षर मंत्र की साधना तीन दिन तक करो उनके मुख से उच्चारित दशाक्षर मंत्र तो मेरी समझ में भली - भाँति आ गया, शेष साधना क्रिया उन्होंने इशारे द्वारा समझा दी । जैसे वज्रासन कैसे लगाया जाता है, धारणी का उच्चारण किस स्वर से किया जाता है, कौन सी मुद्रा प्रयोग में लाई जाए ।
जप के तीन दिन पुरे होने पर मैंने हवन किया । हवन करते हुए मुझे प्रत्यक्ष अनेक चमत्कार देखने मिले । इतना तो मैं कह सकता हूँ कि दशाक्षर मंत्र बहुत शक्तिशाली है । अल्प समय में, थोड़े - से श्रम में सिद्ध हो जाता है और श्री, कीर्ति विजय विभूति को देने वाला हैं ।
ग्यारह दिन तक उस गोम्पा में रहने के बाद मैं कई लामाओं के साथ रावण - ह्रद ( रावण सरोवर ) गया । मानसरोवर से ४ - ५ मील पश्चिम रावण ह्रद हैं । यह १७ मील लम्बा, १३ मी चौड़ा हैं । इसकी परिधि ७७ मील है । इसके चारों ओर पहाड़ हैं । यह वही सरोवर हैं जहाँ पर लंकेश्वर रावण ने भगवान् शिव कि आराधना कि थी । इसलिए इसे रावण ह्रद या राक्षस सरोवर कहा जाता है । गंगाछू नाम कि एक नदी मानसरोवर और राक्षस सरोवर को जोड़ती है । इस नदी द्वारा मानसरोवर का जल राक्षस सरोवर में जाता है । यहाँ भी हंसों के यूथ विचरण करते, केलि करते दिखाई पड़ते है । राक्षस ताल में कई टापू भी है । सरोवर जम जाने पर लोग याक की सवारी पर टापुओं में जाते हैं । राक्षस सरोवर के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीक हैं, किन्तु मुझे वहाँ किसी प्रकार के आध्यात्मिक स्पन्दन का अनुभव नहीं हुआ । राक्षस ताल की एक विशेषता यह हैं कि वह एक ओर अपनी उत्ताल तरंगो से धरती आकाश का भेद मिटता है तो दूसरी ओर शान्त, प्रशान्त सुस्थिर परमहंस बना पड़ा रहता है । कहीं अधिक गहरा, कहीं कम गहरा । मैंने गहराई का तो अनुभव नहीं किया है, किन्तु एक विचित्रता यह देखि कि सरोवर का एक भाग बर्फ से जमा हुआ था । वह स्फटिक मणि के समान चमक रहा था ओर उसपर पवित्र कैलाश पर्वत का प्रतिबिम्ब झलक रहा था ।
मैं दो दिन वहाँ रहा । मुझे एक तिब्बती लामा मिला । जो संस्कृत, प्राकृत, पाली का अच्छा विद्वान था । उसने बतया कि तिब्बती गाथा है कि प्राचीन काल में यहाँ पर राक्षसों का निवास होने के कारण राक्षस सरोवर का जल कोई नहीं पीता । एक बार मानसरोवर कि दो मछलियाँ आपस में लड़ती हुई एक दूसरे का पीछा करती हुई राक्षस सरोवर में जा गिरीं । उस समय से मानसरोवर जा जल राक्षस सरोवर में जाने लगा और जिस स्रोत से वह जल गया उसे गंगा छू कहा गया । मानसरोवर का जल गिरने से राक्षस - सरोवर प्रवित्र हो गया और तभी से इसका जल पिया जाने लगा ।
इन्हीं लामा के साथ एक और लामा था जिसे ' गोमछेन लामा ' कहते थे । उस लामा ने डाकनी सिद्ध कर रखी थी । मारण, मोहन, उच्चाटन, कीलन, विव्देषण और वशीकरण प्रयोग करने में वह सिद्ध - हस्त था । गोमछेन कि भाषा तो मैं नहीं समझ सकता था, किन्तु संस्कृतज्ञ लामा के माध्यम से जो जान सका, वह यह कि गोमछेन का बनाया हुआ कवच पहनने से अथवा इनके द्वारा सिद्ध की गई तलवार धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का शास्त्रघात नहीं होता है । गोमछेन में यह भी शक्ति बताई गई कि वह पहाड़ो की चोटी से दूसरी चोटी पर कूदकर चला जाता था । चढ़ने उतरने की जिल्लत उसे नहीं झेलनी पड़ती है । एक और उस दल में योगी लामा था जिसे ' लुड् गोमपा ' कहते थे । वह उसी दिन प्रातः काल ल्हासा से चलकर दोपहर तक साढ़े चार सो मील दूर स्थित राक्षस तालाब पहुँचा था । उसे लधिमा सिद्धि थी । वह सींक की नोक पर आसान लगाकर बैठ सकता था । दो दिन राक्षस ताल के एक गोम्पा में बिताने के बाद वहीं शान्तानन्द जी आ गए ।
हिमालय मेरी बाहों में
पं देवदत्त शास्त्री।
2)- नादान मेहमान
नेपाल ने अन्तिम तीन सरकार ( प्रधान मंत्री ) मोहन शमशेर जंगबहादुर राणा जिन दिनों वहाँ के कमाण्डर इन - चीफ थे, मैं उनका अतिथि होकर नेपाल गया था । सार्वभौम प्रभुसत्ता संपन्न स्वाधीन देश में पहुंच कर अंग्रेजों की गुलामी से पीटा हुआ मेरा मनोमयूर नाच उठा । स्वाधीन धरा कितना मानसिक उल्लास और प्रभाव भरती है इसका अनुभव सर्वप्रथम मैंने वहीं किया था । सचमुच मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे अपने ही जीवन में अपने देश को सर्वतंत्रस्वतंत्र देखने और स्वतंत्र वातावरण में सुख कि साँस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ ।
नेपाल में मैं शाही मेहमान था । नेपाल के महाराजधिराज पाँच सरकार नाममात्र के थे, शासन - सूत्र राणाओं के हाथ में था । उन दिनों पद्म शमशेर जंगबहादुर राणा प्रधान मंत्री थे,किन्तु राजनीतिक छलछद्म से सर्वथा रहित वे पूरे संत थे । कमाण्डर - इन - चीफ की ही तूती बोलती थी, इसलिए मेरे शाही मेहमान होने में कोई - कसर न थी । बड़े शान और ठाट से मुझे ठहराया गया, मेरी आवभगत की गई ।
एक दिन मैंने एक पहरेदार से दाढ़ी कटवाने के लिए नाई बुला देने के लिए कहा । उस स्वामिभक्त प्रहरी ने तुरंत आज्ञा का पालन किया । मैं बैठा हुआ कुछ लिख रहा था, तो उसने सूचना दी कि नाई आ गया है । मैंने सिर उठा कर देखा तो वहाँ कोई न था । कहाँ है नाई, यह पूछने पर प्रहरी ने इशारा से बताया वह आ रहा है हाथी पर ।
नाई और हाथी पर । मैं सन्न रह गया । देखा तो शाही पोशाक में नाई हाथी से उतर कर मेरी ओर आ रहा है । मैं बड़े पशोपेश में पड़ गया कि दाढ़ी कि बनवाई वैसे अपने देश में आमतौर पर आने दो आने देनी पड़ती है किन्तु हाथीनशीन नाई को सौ दो सौ रुपया भी दिए जायें तो कम होगा - लेकिन अपने राम के पास कुल मिला कर सौ रूपये की भी पूँजी उस समय न थी । शाही मेहमान होना उस समय मुझे खल गया । सारी शान तेजोहीन होती जा रही थी । शर्म, संकोच और भुक्खड़पन की ग्लानि से हृदय बैठा जा रहा था।रह - रह कर परमात्मा पर क्रोध आ रहा था, कि एक नाई की सी भी सम्पदा मुझे देने में परमात्मा तू दिवालिया बन गया । मैं सोच रहा था कि नाई ने आकर बाअदब सलाम किया । उस समय विप्रबुद्धि काम कर गई। दिल तो काँप रहा था, माथा चकरा रहा था किन्तु लेखनी आँय - बाँय - साँय चलती रही । नाई कि ओर बिना देखे ही बाएँ हाथ की छँगुली उसकी ओर बढाते हुए मैंने कहा --- ' इस ऊँगली का नाख़ून बढ़गया है काट दो ।'
नाई ने तुरंत नहन्नी निकल कर छँगुली का नाखून निकाल दिया, बाकी अँगुलियों की मैंने मुठ्ठी बाँध रखी थी । नाखून कटते ही मैंने हाथ खींच लिया और कलम रख कर दाहिने हाथ से ग्यारह रूपये नाई को भेंट किया तो वह मुँह फैला कर खड़ा रह गया ।
कदाचित् उसने भी सोचा होगा कि ऐसा रईस अतिथि है कि सिर्फ एक अंगुली के नाख़ून कि कटाई ग्यारह रुपया देता है यही बाल कटवाता तो न मालूम क्या दे देता ।
मैंने उसे जाने के लिए इशारा किया । वह सलाम कर जब चला गया तो माथे का पसीना पोंछते हुए मैंने सन्तोष कि साँस ली । कुछ मिनट पहले मुझे लग रहा था जैसे सात महारथियों से घिरा हुआ अभिमन्यु व्यूह का भेदन तो न कर सका था,किन्तु मैंने बाजी मार ली और उसी दिन एक रुपया ग्यारह आने खर्च करके शेविंग का सामान लाया और स्वयं दाढ़ी मूँड़ ली ।
नेपाली राजा - परंपरा अतिथि को देवता मान कर उसका उसी प्रकार आतिथ्य करती है जिस प्रकार भारतीय पुराण - परंपरा में अतिथि सेवा की कहानियाँ लिखी मिलती हैं ।
तीन सरकार ने मुझे पाँच सरकार के दर्शन कराए । महाराज त्रिभुवन शाह उनदिनों इस पद पर अभिषिक्त थे|बहुत सुन्दर, सौम्य तरुण थे । उनके मुख में भोलापन के साथ ज्ञान - पिपासा झलकती थी । ऐसा मालूम पड़ता था कि वह मुझ से बहुत कुछ कहना और सुनना चाहते हैं, किन्तु न तो कुछ कह सकते हैं और न सुन सकते हैं। सशंकित और सभीत से नजर आ रहे थे । सादे नेपाली ड्रेस में वे थे । उनके हाथ में बाँस कि एक बंशी थी । पता नहीं क्यों वे जबर्दस्ती गंभीर बने हुए थे । मुश्किल से साथ मिनट मैं उनके पास रहा था ।
जब मैं वहाँ से चलने को हुआ तो राजा कि ओर से मेरी बाकायदा बिदाई हुई । कस्तूरी, रुद्राक्ष और ऊनी कम्बल आदि अनेक प्रकार के वस्त्रों के अतिरिक्त मुझे सदासर्वदा के लिए एक तरुणी परिचारिका और एक परिचारक भी उपहार में दिए गये, जिनका व्ययभार नेपाल सरकार वहां करेगी ।
इस मानवी उपहार कि बात सुनते ही मैं चौंक पड़ा । तीन सरकार से गिड़गिड़ा कर मैंने निवेदन किया कि अपमान न समझा जाए । मेरी मजबूरी है कि मेरे न रहने का ठिकाना, न जीविका का साधन ही है । मैं तो चलता - फिरता घुमक्कड़ हूँ । चलते - चलते जहाँ शाम हो गई वहीं रुक जाता हूँ । जहाँ थकता हूँ वहीं पड़कर सो जाता हूँ, जो कुछ मिल गया खा लेता हूँ; न मिला तो भूखा - प्यासा रह जाता हूँ ।
मेरे बहुत अनुनय, विनय करने के बाद नेपाल सरकार ने मुझ नादान मेहमान पर एहसान करके मानवी उपहार वापस कर लिया किन्तु मुझे द्रव्य इतना दिया कि वहाँ से लौटने पर कश्मीर में रईस बन कर तीन महीना पड़ा रहा ।
स्मृति के हस्ताक्षर
प. देवदत्त शास्त्री
3)-•••••सदेह स्वर्गारोहण•••••
सभ्यता, शिष्टता और नागरिकता की खोल के भीतर खोखली जिन्दगी को भरकर उसका बोझ ढोना मेरे लिये बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे अपना पुराना यायावरी जीवन बहुत प्यारा है। एक समय था न ऋण का सोच न धन की चिन्ता । न आगे नाथ न पीछे पगहा। जहाँ पैर उठ जाते उधर ही चल पड़ता । चलते-चलते चलते जहाँ थक जाता वहीं पड़कर सो जाता । जो कुछ भी मिल जाता उसे अमृत समझकर खा जाता, पत्थर भी पचा जाने की शक्ति थी। जीवन के प्रति कोई मोह न था, मृत्यु से कोई भय न था । आवश्यकतायें, आकांक्षायें नहीं के बराबर थीं, जिज्ञासायें अनन्त थीं। अपनी जिज्ञासाओं की शान्ति के लिये मैं भटकता फिरता था । सत्य तो यह है कि मैं अपनी जिज्ञासाओं के प्रति स्वयं अबोध था । इसीलिए मेरे पर्यटन का न तो कोई उद्देश्य था और न जीवन का कोई लक्ष्य ही था उस समय ।
गया था ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार में नाम लिखाकर पढ़ने, किन्तु कालेज तक पहुँच भी न पाया था कि हर की पैड़ी में एक व्यक्ति ने नीलकण्ठ की भूरि-भूरि प्रशंसा की । सुनकर उसी के साथ ऋषिकेश लक्ष्मणझूला होते हुए नीलकण्ठ चला गया। वहाँ से तीसरे दिन लौटने पर लक्ष्मण झूला में बदरी-केदार की यात्रा पर जाने वाला एक दल मिल गया तो मैं भी उन्हीं के साथ केदार बदरी चला गया । बदरीनाथ में मुझे मालूम हुआ कि वहाँ से ६ मील पर माणा गाँव है जहाँ से भारत की सीमा खत्म होती है और तिब्बत की सीमा प्रारम्भ होती है। मुझे उत्सुकता हुई कि भारत के उत्तरी सीमान्त को देखूॅं।
मैंने साथियों का साथ छोड़ दिया और अकेले माणा की ओर पैर बढ़ा दिये ।
माणा गाँव पहुँचकर मैंने देखा कि गाँव भर के स्त्री, पुरुष बच्चे पाॅंच आदमियों को घेरे हुए रो रहे हैं। मुझे बड़ा कुतूहल हुआ। मैंने वहाँ जाकर लोगों से पूॅंछा तो उन्होंने बताया कि ये लोग पितृश्राद्ध करने जा रहे हैं।
'पितृ श्राद्ध करने जा रहे हैं तो रोने की क्या बात है ?'
मेरे यह पूॅंछने पर एक ने बताया कि आप लोगों की भाँति गया श्राद्ध नहीं है। हमारे यहाँ प्रति पाँचवें वर्ष चार-पाँच गावों के लोग मिलकर अपने-अपने गाँव से एक-एक प्रतिनिधि चुनते हैं जो गाँव भर के मरे हुए लोगों की हड्डियाँ लेकर सतोपथ जाते हैं। उन्हें विदा करते समय इसलिये रो रहे हैं कि जाने वाले फिर लौट कर आते नहीं। इतना दुर्गम मार्ग है कि वहाँ तक पहुँचना ही असंभव है ! कदाचित् कोई पहुँचता भी हो तो लौटता नहीं।
सतोपथ कहाँ है ?'
मेरे यह पूॅंछने पर बताया गया कि यहाँ से पश्चिमी कोने पर अनुमान से तीस-पैंतीस मील पर मल्लापैनखंडा में सतोपथ अवस्थित है। सतोपथ की चार चोटियों में एक चोटी तो इतनी ऊँची है कि सागरमाथा की बराबरी करती है । पुराने जमाने का सुमेरु पर्वत ही सतोपथ है। जिसे सतोपंथ भी कहते हैं। उसके आगे स्वर्गारोहण है ।
स्वर्गारोहण का नाम तो मैंने पढ़ और सुन रखा था, जहाॅं से युधिष्टिर सदेह स्वर्ग पहुँचे थे। मैंने उनसे बड़ी आतुरता से कहा कि इनके साथ मैं भी जाऊँगा। मेरी यह बात उस व्यक्ति ने और लोगों से बतायी तो लोगों ने रोना-धोना बन्द कर दिया मुझे घेर लिया। भले ही वे लोग मुझे सनकी या पागल समझते रहे हों किन्तु मेरे दृढ़ निश्चय को सुनकर सब आश्चर्यचकित थे।
आखिरकार मेरे लिये भी बर्फ पर चलने के लिये मूंज के चप्पल लोहा गड़ा हुआ एक डंडा, एक कम्बल, विशेष प्रकार का सत्तू, हरी चाय और अनाज बोने के ओइर के सामान,एक पोला बाँस आदि संक्षित आवश्यक उपकरण एकत्र कर दिये गये। इन पाँच जीवन्मृत वृद्धों के साथ मुस्कराता हुआ मैं चल पड़ा । मैं यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हम प्रति दिन कितने मील चलते रहे किन्तु तीन दिन तक तो हमें रास्ते में वनस्पति, पशु और पक्षी मिलते रहे । यद्यपि हम किसी बने- बनाये मार्ग से नहीं चल रहे थे, केवल दिशा की सिधाई लेकर गिरि- शिखरों पर चढ़ते-उतरते जा रहे थे । प्रथम तीन दिन का रास्ता कम भयानक नहीं था किन्तु चौथे दिन से हमें हर क्षण मृत्यु का आलिंगन करना पड़ रहा था । डण्डे पर गड़ी हुई लोहे की कील गड़ा-गड़ाकर हम बर्फीले पहाड़ों के कटिप्रदेश, शिखर और वक्ष पर चल रहे थे । तनिक पैर फिसलने पर यह नहीं कहा जा सकता की हमारी अस्थियाँ कहाँ पहुँचतीं । बर्फ ही हमारा ओढ़ना, बिछौना बन गया था। बर्फीली चट्टानों या गुफाओं में हम विश्राम करते । भूख मिटाने के लिये बाँस में चाय, सत्तू और बर्फीला पानी भर कर देर तक खूब हिलाते थे । हिलाते- हिलाते उसके अन्दर ऐसी गर्मी पैदा होती कि चाय सत्तू खौल उठते और गर्म-गर्म हमलोग पीकर भूख, थकावट और शीत को दूर करते थे ।
सातवें दिन हमें एक विचित्र ढंग के वातावरण और प्रकृति का अनुभव करना पड़ा । रुण्ड-मुण्ड रजतमय हिम -शिखरों पर चलते हुए हमें निरन्तर बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा। हर समय हिमानी आँधियाँ चल रही थीं। बर्फ के पहाड़ों को उड़ते हुए हमने वहीं देखा । केवल रात में तीन बजे से संभवतः आठ बजे प्रातः काल तक को छोड़कर शेष समय भयंकर आँधियाँ चलती थीं। हम किसी शिलाखण्ड को पकड़ कर या उसमें अपने को छिपाकर बैठे रहा करते थे। लगभग ढाई दिन तक तूफानों के बीच चलते हुए हमने ऐसी भूमि में चरण रखे जो सुरसा की भाँति किसी समय भी हमें निगलने के लिये मुँह बाये पड़ी हुई थी।
हिमाच्छादित नदियाँ थीं या स्रोत थे हम समझ नहीं सके। हम छह साथियों में से दो तो हिम-तूफानों को भेंट हो चुके थे। एक फिसल कर पता नहीं कहाँ समा गया । दसवें दिन की यात्रा में हम सिर्फ तीन व्यक्ति बचे हिम-सरिताओं की मृगमरीचिका का जाल देखकर हम तीनों ने समझ लिया कि अब सतोपथ इस जीवन में नहीं मिलेगा। यहीं तक द्रौपदी सहित युधिष्ठिर के चारों भाई भी पहुँच पाये थे। इसके बाद सब मृत्यु की भेंट हो गये और अकेले युधिष्ठिर स्वर्गारोहण तक पहुँच पाये थे ।
अपने साथियों से यह कथा सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, फटे हुए, खून चुबचुबाते हुए शरीर की परवाह किये बिना मुख पर मुस्कराहट खेलने लगी। मैंने कहा कि कुछ भी हो हम पाण्डवों से अधिक बलवान् और भाग्यवान् हैं......... जो यहाँ तक आ गये। सम्भव है सतोपथ के भी दर्शन हो जायॅं । किन्तु हमारी यह प्रसन्नता अधिक देर तक न रही। हम जहाँ खड़े थे, सामने की जमीन हिमशिला के बह जाने से खुली हुई पहले से थी । सैकड़ों फिट गहरा गैप था ही, पीछे यही हालत हो गयी । अब हम न आगे जा सकते थे न पीछे लौट सकते थे अन्तिम समय में भगवान का ही सहारा लिया जाता है। आँख मूँद कर नहीं, बल्कि आँख खोलकर हम भगवान का अन्तिम स्मरण कर रहे थे कि सामने के गैप में बहती हुई एक हिमशिला आकर लग गई । तुरन्त हम तीनों उसमें पैर रख कर आगे बढ़ने को आतुर हुए | हम दो तो निकल गये। तीसरे व्यक्ति ने पैर रखा भी न था कि जहाँ खड़ा था वहीं की शिला बह चली, धरती फटी और वह समा गया ।
हम ममता-मोह से परे हो चुके थे। गीता के अनुसार हम उस समय वही पंडित थे, जो मरे हुए और आगे मरने वाले लोगों के लिये शोक नहीं करते हैं।
हम स्वयं अपने को एक प्रकार का मरा हुआ ही समझ रहे थे, अपने को चलती-फिरती लाश समझ कर हम आगे पैर बढ़ा रहे थे । हमारा हर क्षण एक युग बन रहा था। हमें न तो कालज्ञान था, न दिक्कज्ञान था और न हम उस भूमि में आत्मज्ञान ही प्राप्त कर पाये थे । तुहिन सरिताओं को भेंटते और समेटते हुए हमें पूरे तीन दिन लगे। इसके बाद हम एक ऐसी घाटी पर पहुँचे जहाँ हमें धरती के दर्शन हुए । यत्र-तत्र वनस्पति भी दिखाई पड़ी। हम इतने ही दिन के अन्दर जड़ बन चुके थे। हमारी इन्द्रियों के स्रोत सूख-से गये थे। हमारा हृदय ऊसर बन चुका था, न उसमें हर्ष उत्पन्न होता और न विषाद | हमारे अन्दर पहले की-सी प्रगति, तन्मयता, उत्सुकता और जिज्ञासा अब न रही थी। पता नहीं हम चेतन थे या संज्ञा शून्य । हमारा पथ किधर है, यह तो हम दूसरे दिन से ही भूल चुके थे । वस्तुतः उन पाँचों मुमूर्षु वृद्धों के साथ मरने के लिये ही मैं भी चल पड़ा था। घाटी उतरने में हमें दो दिन लगे। तीसरे दिन हम ऐसे प्रदेश में पहुँचे जहाँ की उत्फुल्ल द्रुम-लताओं, मुस्कराती हुई प्रकृति, चह-चहाती हुई चिड़ियों ने हमारे संज्ञाशून्य हृदय में चेतनता, प्रसन्नता का संचार किया | हमारे रोम-रोम में, रग-रग में बिजली की सी लहरें दौड़ गईं । समशीतोष्ण जलवायु हमारे जर्जर प्रताड़ित शरीर के घावों को सहला रहा था । झुकती हुई लता-वल्लरियाँ हमारे अधरों में मुस्कान भर रही थीं। पक्षियों का कलरव हृदय में स्पन्दन भर रहा था, वनश्री सौरभ बिखेर रही थी। एक विचित्र लोक था वह । इससे पूर्व धरती में ऐसा भूमिखण्ड कहीं देखने को नहीं मिला था । हम एक अज्ञात प्रेरणा, अज्ञात शक्ति से सम्पन्न और समृद्ध होकर इस प्रकार चलने लगे मानो पैर में पंख बँध गये हों। सुषमा और सजीवता से सम्पन्न उस पथ -विहीन वन-भूमि में हम ऐसे चल रहे थे मानो हमें कोई रास्ता बतला रहा हो। हमें दो सप्ताह बाद सूर्य के सार्वभौम दर्शन वहीं मिले। लगभग चार बजे अपराह्न में हम चलते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक विस्तृत विशाल सरोवर था।
चारों ओर पर्वतमालाएँ उसे घेरे हुए थीं। शस्यश्यामला धरती, मुस्कराती हुई वनराजि चारों ओर से घेरे हुए उस दिव्य सरोवर का अभिवन्दन कर रही थी। सरोवर तट पर पहुँचकर हम सारी सुधि-बुधि खो गये । हमें ज्ञान नहीं, हम व्यक्त नहीं कर सकते कि हम वहाँ पहुँचकर कितनी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। सचमुच जिसे अनिर्वचनीय आनन्द कहा जाता है वही वहाँ हमें प्राप्त हो रहा था। मेरे शेष साथी ने कहा यही है सतोपथ । न भी हो तब भी उससे बढ़कर सुन्दर कल्पना सतोपथ की नहीं की जा सकती और न उसके ढूँढने का प्रयास ही हमें करना है। उस वृद्ध ने बताया कि परम्परागत सतोपथ के बारे में जो वर्णन हम सुनते आ रहे हैं वह यहीं का है । यह कहकर उसने अपना कम्बल, बाँस आदि किनारे फेंक कर, त्वरा गति से, परम्परा के अनुसार स्नान-तर्पण आदि किया। मैं तट पर बैठा चुपचाप सरोवर का अनन्त वैभव देख रहा था कि मेरे साथी ने सत्तू, चाय घोलते हुए कहा कि 'जल्दी से स्नान कर लो जिससे दिन छिपने से पहले हम जंगल को पार कर लें।' यह सुनते ही जैसे मुझे किसी ने खींचकर तमाचा मारा हो, मैं चोट खाकर गिरा हुआ-सा स्तब्ध रह गया । मनुष्य की ओछी वृत्ति और मोह-जाल की भ्रान्ति का पता ऐसे ही अवसरों पर लगता है । मैं चुप बैठा रहा, उसने फिर टोका तो मैंने कहा कि तुम प्राण देने के लिये आतुर क्यों हो ? अधिक आतुरता हो तो इसी सरोवर में डूबकर निर्वाण प्राप्त कर लो बाबा !
यह सुनते ही बाबा का पारा गरम हो गया । इतने दिन से सुख-दुःख के साथी ने अपने भयंकर क्रोध से मुझे कम्पित कर दिया । जल पीने का इस यात्रा का यह प्रथम सुअवसर था । सरोवर के जल की उपमा किससे दी जाय। अमृत को सुना है, देखा नहीं । यदि अमृत मीठा होता है तब तो सरोवर का जल अमृत नहीं हो सकता और यदि अमृत जरा-मरण से रहित बनाता है तब तो निःसन्देह वह जल अमृत है। वह मनुष्यों नहीं देवताओं द्वारा अवश्य उपभोग किया जाता होगा। पानी पीते ही मेरी थकावट नस-नस से निकल गई । मुझे विचित्र प्रकार की आध्यात्मिक तृप्ति का अनुभव हुआ। इतना स्वच्छ जल कहीं देखने को नहीं मिला। वह पारदर्शी दर्पण की भाँति चमक रहा था। न तो उसमें कमल थे, न सेवार, न अन्य कोई तृण-शाद्बल थे । मछलियाँ पर्याप्त थीं और जितनी थीं उतने ही प्रकार की, उतने ही रंग की। दूर तक प्रवेश कर के मैंने अवगाहन किया, खूब नहाया और फिर सन्ध्या-तर्पण किया। उसके बाद बाहर निकला ।
मेरा साथी अपना बाँस संभाले चलने के लिये तैयार था। मैंने बहुत समझाया कि दो एक दिन यहाँ ठहर कर विश्राम किया जाय, किन्तु उसे घर का भूत सवार था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जीवन का अलभ्य श्रेय जब अनायास मिल रहा है तो उसका उपयोग भी किया जाय। यहाँ घूम फिर कर देखा जाय, सही सलामत लौटकर पहुँच गये तो जीवन की एक अप्रतिम घटना बनकर यह यात्रा सदैव गति और प्रेरणा देती रहेगी, और नहीं बचे तो संतोष के साथ हिमालय में विलीन हो जायेंगे। मेरी प्रबल इच्छा थी कि सरोवर के चारों ओर परिक्रमा कर के पता लगाया जाय कि उसका व्यास कितना है । कहाँ क्या उल्लेखनीय है, यहाँ का वनप्रान्त कैसा है ? किन्तु साथी ऐसा जड़ मिला था कि उसके सामने मेरी एक भी नहीं चलती थी, साथ ही उसका साथ भी न छोड़ने का मोह समाया हुआ था।
हम दोनों के विवाद का परिणाम यह निकला कि रातभर तक ठहरने को वह राजी हो गया। मैंने भी अपना बाँस सँभाला। सत्तू और चाय का घोल तैयार कर पिया रात भर हम लोग बड़े सुख से सोते रहे। इतने दिनों की यात्रा में सोने का यह पहला ही अवसर था। प्रातः शौच-स्नान से निवृत्त होते-होते सूर्योदय हो गया।
सूर्य की स्वर्णिम किरणें सरोवर के जल में पड़कर अनन्त इन्द्र-धनुषों का सर्जन कर रही थीं।
मेरे वृद्ध साथी ने सामने चमकते हुए एक पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही स्वर्गारोहण है। स्वर्गारोहण के छाया दर्शन कर मैं आत्मविभोर हो उठा। पूॅंछने पर उसने वहाँ से उसकी दूरी का अनुमान बारह मील के लगभग बताया। इतना नजदीक स्वर्गरोहण है यह जानकर स्वर्गारोहण तक जाने की मेरी उत्कण्ठा तीव्र हो उठी। मैंने अपना इरादा उससे जाहिर किया तो वह फिर बौखला उठा और व्यंग कसता हुआ बोला- स्वर्गारोहण तक आज तक किसी आदमी के पैर नहीं पहुँच सके तुम्हीं एक धरती के देवता हो जो वहाँ पहुँच जाओगे ?
स्वर्गारोहण तक चलने का मैं जितना अनुनय- अनुरोध करता मेरा साथी उतना ही उखड़ता, खीजता था। उसकी ऐसी मनोवृत्ति देखकर मैं चुप हो गया । इतने में वहाँ पर अकस्मात् एक और पहाड़ी आदमी आ पहुँचा। उसने मुझसे पहाड़ी भाषा में कुछ कहा जिसका जवाब मेरे सहपाठी ने दिया । उसने हिन्दी में बोलते हुए मुझसे कहा कि तुम स्वर्गारोहण चलना चाहो तो मैं तुम्हें ले चल सकता हूँ ।
'लेकिन लौटने में भी तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा ।'
यह सुनकर हँसता हुआ मेरा साथी बोला- 'वहाँ पहुँच सकोगे भी कि लौटने की ही शर्त और फिक्र है ?'
मैं बूढ़े साथी से विवाद नहीं करना चाहता था। बल्कि अब तो मुझे यह लगता था कि कब इसका साथ छोडूॅं । नवागन्तुक को भी इतनी जल्दी थी कि उसने बात न बढ़ाकर मुझे चलने का इशारा किया । मेरा साथी पूर्व की ओर चल पड़ा और मैं पश्चिमोत्तर दिशा की ओर ।
सतोपथ से स्वर्गारोहण की विराट रजतमयी काया के तीन शृङ्ग आकाश को स्पर्श करते हुए साफ झलक रहे थे ।
अन्दाज से हम ६ मील भी न चले होंगे कि वनश्री ने हमारा साथ छोड़ दिया और रजतमय पर्वत-शिखरों की श्रृंखलायें हमारे सामने आने लगीं। वही विपद, वही परेशानियाँ जिनसे हम पूर्वपरिचित थे, हमें पग-पग पर रोकती सी जान पड़ती थीं। मेरा नया साथी देखने में आदमी किन्तु चाल-ढाल, व्यवहार में एक अद्भुत जीव जान पड़ा। दुर्गम पहाड़, अभेद्य मार्ग में वह इस तरह चल और बढ़ रहा था जैसे बहता हुआ पानी और उड़ता हुआ पक्षी या कूदता हुआ बन्दर चलने के बाद वह बिल्कुल मौन हो गया था। मैं उससे पिछड़ जाता कहीं फँस जाता अथवा गिरने-मरने की स्थिति में होता तो बिजली की भाँति लपक कर वह इशारा करता और सहारा देता उसके पास खाने-पीने, ओढ़ने के सामानों की कौन कहे बर्फीले पहाड़ों पर चलने के लिए पैर में जूते हाथ में छड़ी तक न थी। पहले तो मैंने स्वर्गारोहण जाने की उत्कण्ठा में विमुग्ध होने से उसके उस फक्कड़पन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था किन्तु रास्ते में उसका रंग-ढंग, रवैया देखकर मुझमें भय, और आशंका समा गई। मुसीबत तो यह थी लौटना भी संभव न था ।
माणा से सतोपथ तक का मार्ग जितना विपद्ग्रस्त था उससे सैकड़ों गुना कठिन, विपद्ग्रस्त मार्ग स्वर्गारोहण का था। लेकिन आश्चर्य है कि नंगे पाँव, नंगे सिर, बिना- लाठी छड़ी के वह व्यक्ति उस समय पवनपुत्र बना चल रहा था और मुझे भी उड़ाये लिये जा रहा था। कई मौके ऐसे आये कि पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरने के लिये बिहंग ढाल मिले किन्तु मेरा हाथ पकड़ कर वह इस तरह फिसलता मानो पहाड़ी झरना गिर रहा हो। अनेक अवसर ऐसे आये कि मैं उसका साथ निभाने में बिलकुल असमर्थ हो गया। आगे बढ़ने से मैं साफ इन्कार कर देता तो वह केवल मुस्करा देता था और हाथ पकड़कर मुझे बलात् ढकेल देता था। एक जगह ऐसा हुआ कि भयंकर हिमनद रास्ता रोके हुए मिला।
मुझे डर लगा कि कहीं यह दानव इसमें मुझे कुदा न दे मैं पिछलकर रुका तो मुस्कुराता वह दूसरी दिशा की ओर मुड़ा और मुझे शीघ्र पीछे चलने का उसने इशारा किया। जब कभी वह मेरा हाथ पकड़ता तो मुझे क्षण भर के लिये ऐसा एहसास होता कि बिजली का करेण्ट छू गया। एक बार उसने मुझे थामा तो भय से मैंने आँखें मूँद ली । मैं चल रहा हूँ इतना तो बोध मुझे था किन्तु वह न मेरा हाथ छोड़ता और न मैं आँख खोलता। वहाँ से किस मार्ग से और कैसे वह मुझे ले गया यह जान न सका, देख न सका। जब वह मेरा हाथ छोड़ कर दूर खड़ा हो गया तो मैंने आँखें खोलीं। मेरे सामने विराट स्वर्गारोहण था और मैं उसके चरणों के नीचे खड़ा हुआ था।
स्वर्गारोहण यही है यह अनुमान करने में मुझे विलम्ब न लगा, सीढ़ीनुमा वह महान् गिरि ओर से छोर तक कहकही दीवार की तरह खड़ा था । ऊपर कहाँ तक ऊँचा है यह अनुमान करना मेरे लिये कठिन रहा । ऐसा मालूम पड़ता था कि वह आसमान के भीतर तक घुसा हुआ है। नीचे से ऊपर तक, ओर से छोर तक वह निरा चाँदी का-सा जान पड़ता था। एक भी वनस्पति, एक भी पक्षी के दर्शन वहाँ न हुए । जहाँ तक दृष्टि जाती थी, वहाँ तक फैली हुई सीढ़ियाँ-सी बनी हुई थीं। एक के ऊपर एक सीढ़ी बनी हुई थी। वह पहाड़ एक विराट सीढ़ी-सी जान पड़ता था । पहली सीढ़ी मेरे कमर तक की ऊँचाई से शुरू थी, दूसरी उसके ऊपर लगभग सौ डेढ़ सौ गज की ऊँचाई पर थी। तीसरी शायद उससे फर्लाङ्ग भर ऊँची थी, इसी प्रकार उन सीढ़ियों को मैंने अपने अनुमान से समझा ।
मैंने उस विचित्र मानव से पूॅंछा- 'क्या यही स्वर्गारोहण है ?' उसने मुस्करा कर 'हाँ' कहा। मैंने श्रद्धा से मस्तक झुका दिया। उस समय सूर्य अस्त हो रहा था । वातावरण बड़ा शान्त था, आकाश स्वच्छ था। मैंने जी भर कर स्वर्गारोहण के दर्शन किये। वह पर्वत नहीं विराट ब्रहा-सा प्रतीत हो रहा था।
अभी तक सतोपथ को ही मैं धरती का अद्वितीय स्थान समझ रहा था किन्तु स्वर्गारोहण धरती और आकाश दोनों से भिन्न निश्चय स्वर्गीय स्थान था। मुझे महाभारत की कथा याद आ गई कि धर्मराज युधिष्ठिर यहीं से सीधे स्वर्ग गये थे। मैं सोचने लगा-वह विमान से स्वर्ग गये होंगें। आकाश में स्वर्ग है यह तो कल्पना मात्र है किसी ने देखा नहीं। पत्नी और भाइयों के वियोग का भार वहन करते हुए धर्मराज यहाँ तक अवश्य आये होंगे। इसके बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले होंगे तो उन्होंने इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ना आरॅंभ किया होगा,सम्भव है एक दो सीढ़ी चढ़ने के बाद कूद कर प्राण गँवायें होंगे या हिमन का स्पर्श कर गल गये होंगे।
मैं अपने मन ही मन ऐसी ही कल्पनायें कर रहा था। मेरा साथी शान्त खड़ा हुआ मुझे देख रहा था। ऐसी ऊल-जलूल बातें सोचते-सोचते मेरे मन में आया कि मैं भी एक सीढ़ी का स्पर्श कर स्वर्गारोहण को प्रणाम करूॅं। यह सोच कर ज्यों ही दाहिने हाॅंथ से मैंने पहली सीढ़ी को हुआ तो जैसे डी. सी. करेण्ट छू जाय, एक जोर का झटका लगा। मैं पीछे हटकर खड़ा हो गया। मेरा साथी मुस्कराने लगा। स्वर्गारोहण को प्रस्थान करने से वहाँ तक पहुँचने के बाद पहली बार उसका मुँह खुला वह बोला 'दोनों हाथ रखो।' मैंने दोनों हाॅंथ ज्यों ही रखे कि एकाएक जैसे मुझे किसी ने उछाल दिया और उछलकर दूसरी सीढ़ी में करवट के बल गिर कर मैं उसी में चिपक गया। अजीब परेशानी में पड़ गया मैं । हिलने-डुलने की बहुत कोशिश की किन्तु एक सूत भी न खसक सका। मुझे चिपका हुए देखकर वह आदमी चलने के लिये तड़तड़ाने लगा। मैं विवश प्रार्थना करता तो वह और भी जोर मारता। मैंने सोचा कि अब तो बचना असंभव है, मरना निश्चित है । आँखें मूँद कर राम-राम जपने लगा कि इससे पहले मेरा वह दूसरा साथी भी चला गया वहाॅं से। चार पॉंच-मिनट तक मैं नेत्र बन्द किये भजन करता रहा।
मेरा यह राम-नाम-जप विवशता का था। मुझे पता नहीं कब नींद आ गयी या मैं बेहोश हो गया और उसके बाद क्या हुआ कुछ स्मरण नहीं । दूसरे दिन प्रातः सूर्य की किरणें जब निकल रही थीं तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सतोपथ में हूॅं और सरोवर की ओर चल रहा हूँ। मैं अचकचा कर अपने को तथा इधर-उधर देखने लगा। मुझे अपने पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे याद आया कि शाम को तो मैं स्वर्गारोहण की सीढ़ी पर चिपका हुआ था। मैं एक प्रकार से पागल-सा हो रहा था । सरोवर के तट पर पहुँचते वही विचित्र साथी वहाँ बैठा हुआ मिला । उसने बड़े इतमिनान से कहा 'तुम आ गये। तब मुझे होश हुआ ।
मैं उससे पूँछ रहा था कि मैं तो चिपक गया था, तुम छोड़कर चले आये थे, फिर कैसे मैं छूटा और कैसे यहाँ पहुँच गया ।' उसने कुछ जवाब न देकर कहा-जल्दी से नहा लो, पानी पी लो । तब मुझे याद आया कि मेरा कम्बल, बाँस, डंडा आदि सब तो स्वर्गारोहण ही में रह गये । मैं अत्यन्त अधीर हो उठा और उससे कहने लगा कि तुम मुझे अपने घर ले चलो । वहाँ कुछ दिन रहने के मुझे बद्री धाम का रास्ता बतला देना या किसी का साथ कर देना । किन्तु वह वज्र-पुरुष अपनी ही जोत रहा था। कह रहा था 'जल्दी नहाओ मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा जहाँ से आये हो।' मैं बार-बार कहता कि हम दोनों नहीं बचेंगे एक दिन का मार्ग तो है नहीं किन्तु वह मेरी एक न सुनता।अब वही मेरा आधार था । उसका कहना मानने के सिवा कोई चारा नहीं था।
नहा-धोकर गीले वस्त्र पहन कर मैं चल पड़ा उसके साथ । परमात्मा जाने कि किस मार्ग से वह मुझे ले गया कि सुबह का चला हुआ तीसरे पहर मैं माणा गाँव के समीप पहुँच गया । वही पहाड़, वही नदियाँ, वही हवाएँ किन्तु इस बार मुझे कुछ भी अनुभव न हुआ । साधारण हिम वायु का अनुभव हुआ । साधारण कष्ट मिला, किन्तु वह किस मार्ग से ले गया कि पूरा दिन भी न लगा मैं पहुँच गया।
माणा गाँव दिखाई पड़ने लगा तो उसने बताया कि यही है माणा गाँव अब तुम जाओ। यह कहकर वह लौटने लगा तो मैंने कहा कि 'तुम अब कहाँ जाओगे ?' उसने कहा 'अपने गाँव ।" मैंने कहा आज यहीं रह जाओ। किन्तु शायद इतनी बात सुनने को भी वह राजी न था। मैं खड़ा देखता रहा और वह चला गया ।
माणा आकर मैंने लोगों से सारा किस्सा बताया तो लोग कहने लगे । साक्षात् भगवान् था । कोई कहता कोई ऋषि मुनि होगा । इसमें सन्देह नहीं वह अवश्य कोई विशेष शक्ति रही जो मनुष्य शक्ति से कहीं अधिक उच्च थी। उस दिन तो मैं माणा में ही रहा दूसरे दिन बद्रीनाथ जाकर रावल से कम्बल और उधार रुपया लेकर मैं अपने घर चला आया ।
मेरी यह यात्रा जीवन की सर्वोत्तम और-भयंकर रोमांचकारी घटना है। इसकी याद कर मैं अब भी सहम जाता हूॅं साथ ही अपनी पीठ भी ठोकता हूँ इसलिये कि जहाँ से युधिष्ठिर नहीं लौट सके वहाँ से मैं लौट आया ।
स्मृति के हस्ताक्षर
पण्डित देवदत्त शास्त्री
4)•••••हिममानव से भेंट•••••
भूल न सकूँगा कभी अपने उस यायावर जीवन को । जब न मरने का भय था और न जीने की लालसा।कामना सिर्फ यही रहती कि चलता रहूँ, घूमता रहूँ, नित्य नवीनता का अनुभव करता रहूँ और अपने देश की प्रकृति की विचित्रता, विविधता की जानकारी प्राप्त करूँ।
मेरी इस कामना को तीव्रतर बनाने में, मेरी इच्छाओं को प्रज्वलित करने में ईंधन का काम दिया डाॅक्टर स्वामी शान्तानन्द सरस्वती महाराज ने | वह विद्वान् संन्यासी जितना विद्वान् उससे अधिक त्यागी और सर्वाधिक मस्त था। मैं कह नहीं सकता कि उनके मिल जाने से मेरी पूर्णता हुई या मेरे मिल जाने से उनकी कमी पूरी हुई। कुछ भी हो हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए थे ।
मुझे वे मिले थे कश्मीर की शङ्कराचार्य पहाड़ी में । मेरी वह कश्मीर यात्रा तीसरी और अन्तिम थी, स्वामी जी ने मुझे उकसाया अमरनाथ चलने के लिये जब कि अभी अमरनाथ यात्रा का समय नहीं था ।
हम दोनों चल पड़े। दोनों के पास सीमित साधन थे । एक मानी में हम सब साधनहीन थे ।अमरनाथ गुफा जाने के लिये हम लोग पहलगाम तक तो ठीक रास्ते से गये किन्तु वहाँ से 'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः' वाली कहावत चरितार्थ हुई। बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से होकर चलता, जीवन का, प्रकृति का और विपत्तियों का अनुभव प्राप्त करना ही शायद हमलोगों का अभीष्ट था। स्वामी जी प्रयोगवादी स्वभाव के थे। जीवन की नन्हीं-मुन्नी बातों में, कार्यों में वे नये प्रयोग करने में अभ्यस्त थे। उनके प्रयोगवाद ने मुझे भी चक्कर में फँसा दिया ।
जो कुछ कपड़े पहने हुए थे उनके अलावा एक कम्बल एक डंडा और पैर में जूते छोड़कर और कुछ भी हमारे पास न था । जहाँ कहीं फल, फूल मिल जाते खा लिया करते थे। स्वामीजी कंद-मूल के पारखी थे-जहाँ तक कंद-मूल मिलते वे हर हिकमत से उखाड़ कर ले आते और दोनों कच्चा चबा जाते ।
हम हिमाच्छादित पर्वतमाला के कहीं चरणों के नीचे चलते कभी उनकी कटि पर, कभी पीठ पर और कहीं हमें उनके शिखर पर चढ़ना पड़ जाता था ।
वनस्पति बहुत कम मिलती, पशु-पक्षी भी बहुत कम दिखाई पड़ते। हम बिना किसी दिशा ज्ञान के चलते, जहाँ थक जाते वहीं दुबक कर सो जाते। कई मौके तो ऐसे भी आये कि जाड़े के मारे आइसक्रीम बन गए ।
हम दोनों ने यह समझ लिया कि अमरनाथ के दर्शन तो अब मिलेंगे नहीं किन्तु उस भूमि के दर्शन हम कर रहे थे, जहाँ शायद कोई जाता नहीं। दो दिन से कुछ भी खाने को न मिला, पानी भी जहाँ कहीं मिलता वह मानो हिमप्रलय की प्रतीक्षा करता हो । तीसरे दिन हमें एक घाटी मिली वहाँ वनस्पति भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ी, चिड़ियाँ भी उड़ती हुई नजर आईं। एक झरना मिला जिसके आस-पास एक ऐसी हरी-हरी लता बौड़ी हुई थी जिसमें मकोइया की तरह लाल-लाल पके हुए सुन्दर फल गुच्छे के गुच्छे लदे हुए थे ।
स्वामीजी ने कहा कि कुदरत ने खाने के लिये फल तो दिया, भले ही यह जहर हो । अब तो इसे खाना ही चाहिए। हम दोनों फलों को तोड़ने लगे। मैं खाने जा रहा था कि स्वामी जी ने रोक कर कहा, पहले मुझे खाने दो पता नहीं कैसा फल है-उन्होंने दस बीस फल एक साथ मुख में रखकर बताया बहुत मीठे और स्वादिष्ट फल हैं-
यह बात दूसरी है कि इस मधुरता में विष छिपा हो । मैंने कहा स्वामीजी मुझे तो खाने दीजिये, मरेंगे तो साथ ही मरें।
यदि बिना खाये मैं जीवित रह गया तो अकेले तड़प-तड़प कर मरने से बेहतर है कि हम दोनों एक-दूसरे को देखते हुए मरें।
हम दोनों ने भर पेट फल खाया, झरने का पानी पिया और जेब में जितने फल भरे जा सकते हैं उतने तोड़ कर भर लिये। आगे चलने पर एक गुफा मिली जिसके द्वार पर जटा खोले हुए एक महात्मा मिले। कई दिन बाद मनुष्य जाति को देखकर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह महात्मा हमारी भाषा से सर्वथा अपरिचित थे, हम कुछ कहते तो वे अपनी भाषा में कुछ और कहते। स्वामी शान्तानन्द तिब्बती, लद्दाखी भाषाओं से परिचित रहे, वे उनसे रुक-रुक कर उनकी भाषा में बोलने लगे ।
उस परिचय से हमें यह मालूम हुआ कि हम अमरनाथ के बजाय लद्दाख की ओर जा रहे हैं। और जो दिशा या कुमार्ग अपनाया है, उससे इस जन्म में पहुँच ही नहीं सकते ।
उन महात्मा जी के बतलाने पर हम दोनों वहाँ से ५ मील दूर एक नाला देखने गए। सुबह के चले शाम को पहुँचे। उस नाले का नाम महात्मा जी ने 'सीताझ्योरी' बतलाया, उसकी विशेषता यह रही कि दुनियाँ की किसी भाषा में यह कहा जाय कि 'सीताजी रामजी आए' तो नाले का प्रवाह कुछ तेज हो जाता था और बीच में यदि यह कह दिया जाय कि रावण आया है तो प्रवाह मध्यम हो जाता था। स्वामी शान्तानन्दजी जितनी भाषायें जानते थे सबका उपयोग उस समय उन्होंने किया था— उस नाले का विज्ञान आज तक किसी की समझ में न आया ।
रात हो जाने से न तो हम आगे जा सकते थे और न पीछे लौट सकते थे, इसलिए उसी नाले का पानी पीकर हमने एक शिला में मुँह छिपाकर रात बितायी ।
सबेरे उठकर चलने को हुए कि हम दोनों जहाँ बैठे थे वहीं इस प्रकार अकड़े हुए बैठे रहे मानों किसी ने हमें गाड़ दिया है।
दोपहर तक अकड़े बैठे रहने के बाद जब धूप लगी तब कहीं हम सीधे हो पाये। वहाँ से चलने को हुए तो दिग्भ्रम हो गया, हम वस्तुतः आगे जाना चाहते थे किन्तु अज्ञान से पीछे लौट पड़े किन्तु पहले के मार्ग से नहीं। हम पहाड़ों की छोटी-मोटी ऊँचाई नापते धीरे-धीरे चढ़ते-उतरते चल रहे थे कि अचानक यती -यती की पुकार हमें सुनाई पड़ी-हम भयभीत होकर इधर-उधर देखने लगे, तो अकस्मात् हमारी दृष्टि एक हिमाच्छादित पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो १० फुट से कम लम्बा न होगा, सारा शरीर नंगा किन्तु बड़े-बड़े बालों से ढका हुआ था - और उसका त्रिभुजाकार शिर बड़ा भयावना था—वह वनमानुष शायद हमारे पास से ही गुजरा था किन्तु उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह गया छूमन्तर हो गया । हमने जब होश संभाला तो देखा कि बर्फ पर उसके पैरों के निशान बने हुए थे। उसके पैर की पाँचों अंगुलियाँ बर्फ पर साफ उपटी हुई थीं।
हमने समझा यह मनुष्य नहीं राक्षस होगा, जैसा कि पुराणों में राक्षसों के रूप, गुण, कर्म के वर्णन मिलते हैं, वही उसके भी रहे। मनुष्य और पशु की कौन कहे चिड़ियाँ भी उड़कर इतनी तेजी से पर्वत शिखर पर नहीं जा सकती । वह तो अग्निबाण बनकर छूमन्तर हो गया था।
सचमुच हम अधिक भयत्रस्त हो चुके थे। चुपचाप खड़े काँप रहे थे। थोड़ी देर में स्वामी जी ने पूॅंछा कि यती- यती की आवाज किसने दी है। हम सोच रहे थे कि कोई अदृश्य शक्ति ने हमारे बचाव के लिये यह ध्वनि की होगी, कि इतने में ढाल पर से वही महात्मा आते हुए हमें दिखाई पड़े तो हम चिल्ला उठे ।
उन्होंने दूर से ही हमें आश्वासन दिया - कुछ देर बाद वह हमारे पास आये तो उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि नरभक्षी यती के ग्रास बनने से हम लोग बच गये। स्वामीजी ने पूॅंछा कि यती क्या है तो उन्होंने बताया कि बर्फ के पहाड़ों का यह नरभक्षी मानव है । इसमें अपार शक्ति और साहस रहता है। मनुष्य,पशु जो भी इसके हाथ लगता है झपट कर उठा भागता है। वायु की भाॅंति इसकी गति अबाध है, यह अजेय प्राणी है।
यह सब सुनकर हमारा सारा जुनून शान्त हो गया, हम श्रीनगर लौटने के लिये उतावले हो गये। महात्मा जी के साथ चल कर शाम को उनकी गुफा में पहुँच कर रात में वहीं विश्राम किया । सवेरे महात्मा ने हमें दिशा का बोध कराया और किसी पेड़ या लता की पतली-पतली दो जड़े देकर कहा कि इसमें से एक की एक अंगुल जड़ खा लेने से भूख-प्यास तीन दिन तक न लगेगी और दूसरी की एक अंगुल जड़ खा लेने से भूख प्यास खुल जाएगी। हमने भूख प्यास न लगने वाली जड़ वहीं खायी और प्रस्थान किया । सत्रह दिन बाद श्रीनगर लौटने पर दूसरी जड़ी जब खायी तो भूख प्यास खुल गई । श्रीनगर,आने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमने हिममानव से मुलाकात की थी।
**
स्मृति के हस्ताक्षर
पण्डित देवदत्त शास्त्री
5) भाग-2 "आग्नेय तीर्थ हिङ्गलाज- पंडित देवदत्त शास्त्री"
जय हिङ्गलाज
हिंगलाज की मेरी यात्रा ‘आ बैल मुझे मार’ की तरह रही। तीनमहीना कश्मीर की सुखद सुषमाका रसपान करने के बाद शीतल-मन्द-सुगन्धपवन का स्पर्श प्राप्त करनेके बाद एकाएक अग्निकुण्ड में कूद पड़ा। यह मेरा बहशीपन ही था, क्योंकि मेरी कोई कामना नहीं थी। किसी कामना की पूर्तिके लिए देवी के दर्शनों के लिए कोई मनोती नहीं मान रखी थी और न धर्म-प्राण बनकर ही तीर्थ यात्रा के लिए पैर उठाये थे ।
नागनाथ के अखाड़े में कुल २७ यात्री एकत्र हो गये थे, उनमें एकस्त्री-पुरुषका जोड़ा भी था। पतिका नाम जीवराज करसनजी साँचोराथा और पत्नीका नाम जयावेन था । जीवराज भाईने तीसरी शादी कर जयावेनको पाया था । जयावेनकी उम्र २७ वर्षकी थी और जीवराज भाई की उम्र ५४ वर्षकी थी। दस वर्ष शादीको हो गये थे, किंतु जयावेन कीगोद नहीं भरी थी । सन्तान सुख प्राप्त करने, पुत्र का मुख देखने की मनौती मान रखी थी दोनोंने । कोई पुत्र-पुत्री न होनेपर हिंगलाज दर्शन के लिएआये थे ।
हम सत्ताईस तीर्थयात्रियों के अलावा एक छड़ीदार, दो ऊंटवाले सबमिलाकर तीस मानव प्राणी थे । ऊँटनी ‘गुलबदन’ और ऊँट ‘तूफान’ कोभी मिलाकर कुल ३२ प्राणी थे, जिनमें जयाबेन और गुलबदन दो स्त्रीलिंग शेष पुल्लिंग थे ।दोनों ऊँटोंपर सामान लाद दिया गया। तीसरे पहरके चार बजे थे,सब लोग अपनी-अपनी सुराही कन्धेपर लटकाकर ‘जय माता हिंगलाज’का उच्चघोष कर चल पड़े। कराची से बाहर निकलने पर खेत मिले, बंजरभूमि मिली, कुछ रेतीली, भुरभुरी जमीन मिली। झाड़ियां, भाड़, कांटे,कड़ मिले। बड़ा उत्साह था हम सब लोगों में । आषाढ़का महीना था ।बादल न बदली, न बूंद न लू-लपट । निरभ्र, निर्लिप्त आकाश। उछाह भरा वह वर्तमान बड़ा सुखद और सुनहला लग रहा था। भविष्य को कोई चिन्ता न थी । लगभग तीन-चार मील चलने के बाद कुश कण्टकाकीर्ण पथ मिला । कांटे चुभनेपर सी-सीकर आगे बढ़ते, दर्भ की नोक गड़ने परबल्लसे खून निकल पड़ता था, किंतु कोई हरकत नहीं, माता हिंगलाज कीजय बोलकर आगे बढ़ जाते । जयाबेनको गोद भर जानेका पक्का विश्वास था, इसलिए उसका उछाह हम सबसे छब्बीस दुगुन बावन था। वह तितली-की तरह फुदकती, बिजलीकी तरह चमकती, लह्रोंकी तरह इठलाती चलरही थी । झाड़ियाँ उसकी साड़ी पकड़कर जब रोक लेतीं तो वह ‘उई माँ’कहकर बैठ जाती और जीवराज भाई दौड़कर उसे झाड़ियोंके बाहुपाश सेमुक्त कराते । वह फिर फुदकती, उड़ती हुई आगे बढ़ती और कांटे चुभने पर हाय ! हाय ! कर लोट-पोट हो जाती तब तो कुछ क्षणोंके लिए सब लोगों को रुकना पड़ता था ।
उमङ्गों भरी राह चलते-चलते देखा सूर्य समुद्र में डुबकी लगा रहाहै। प्रकृति सान्ध्य परिधान धारण किये निशा की बाट जोह रही है।सूर्यास्त होते-होते हम लोग ‘हाव’ नदी के किनारे पहुँच गये । यही पहलापड़ाव था, उस यात्राका और वास्तविक तीर्थ-यात्रा यहीं से प्रारम्भ होती थी।
‘हाव’ नदी के इस पार सिन्ध प्रदेश की सीमा समाप्त होती है औरनदी पार करनेपर बलूचिस्तान के लासबेला राज्यकी सीमा प्रारम्भ होतीहै। लासवेला स्वाधीन राज्य था, उसी राज्य में देवी हिंगलाजकी अवस्थितिहै। बलूची हृष्ट-पुष्ट लम्बे-तड़ंगे शानदार जिस्म के घनी और स्वाभिमानीव्यक्तित्वके पानीदार व्यक्ति होते हैं। गुलबदन का मालिक शेरमुहम्मदसाढ़े ६ फुटका चालीस वर्षीय बाँका बल्लोच था और तूफान का मालिककासिम भीमकाय साठ वर्षीय पट्टा था। वह ‘साठा सो पाठा’ की कहावतचरितार्थ कर रहा था। दोनोंके हाथ में चमचमाते हुए फरसे थे। दोनों धीर,गम्भीर, मितभाषी और अतिशय विनम्र थे। अपनी-अपनी ऊँचाईके अनुसारवे चरित्र के भी ऊँचे थे ।ऊँटों से सामान उतार दिया गया । सबने अपनी-अपनी गठरी मुठरीअलग कर लो। मेरे पास बोरों और बोरियों में सुव्यवस्थित सामान इतना था कि उस सामान के कारण मैं सभी यात्रियों से समृद्ध और सम्पन्न बन गया था। यदि साधुवेला तीर्थ मुझे सम्पन्न न बनाता तो मैं ही सबसे निकृष्ट, मुफलिस मुसाफिर होता । चना चबाता, रोटी नसीब न होती और अगर चना समाप्त हो जाता तो वीरान रेगिस्तान में 'हुं फट् स्वाहा हो जाता।
छड़ीदार ने अपनी भाषा में कुछ पढ़कर छड़ी गाड़ दी, फिर गाँजा काभोग लगाकर चिलमको मुँह में सटाकर ऐसा कश खींचा कि चिलम आगउगलने लगी। हमारे पुरोहितजी के नेत्र आग्नेय हो गये। सब लोगोंने अपने-अपने ढङ्गका जल-पान किया, किसी ने चाय-चिवड़ा लिया, किसीने मोदकफोड़े, हमने मेवा खाया । प्रातः ३ बजेके लगभग कासिम और शेर मुहम्मद अपने-अपने ऊँटोंको उठ बैठ कराने लगे। छड़ीदारने हाँक लगाई। सब यात्री तैयार होगये । हाव नदी में स्नान किया। पण्डा सबके लिए एक-एक गेरुए रंगवस्त्र के टुकड़े हाथमें लिए था। हम सब उसको चारों ओरसे घेरकर खड़ेथे। उसने कड़कती आवाज में हम लोगों को यह शपथ दिलायी कि 'जबतक माता हिंगलाज के दर्शन कर पुनः यहाँ नहीं लौटेंगे, तबतक हम लोगसंन्यास धर्मके नियमों का पालन करेंगे। एक दूसरेकी यथाशक्ति सहायताकरेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, निन्दा के भाव हृदयमें नहीं रखेंगे, किंतु किसी भी हालत में अपनी सुराहीका पानी किसी दूसरे को नहीं देंगे, यहाँ तक कि पति-पत्नी को,पत्नी पतिको, पुत्र- पिताको, पिता-पुत्रको, मां-बेटेको, बेटा माँ को भी अपनी सुराहीका पानी नहीं देगा, जो इस नियमका उल्लंघन करेगा उसकी मृत्युनिश्चित होगी ।'
यह शपथ दिलाने के बाद उस तीर्थ पुरोहितने प्रत्येक यात्री के सिरपरगेरुए रङ्गके वस्त्र के टुकड़े बांध दिये, तदनन्तर यात्रियों में से एक आदमी कोप्रधान चुन लेनेका आह्वान किया। कदाचित् मेरे पास सबसे अधिक खाद्य-सामग्री होने के कारण मुझे विशिष्ट, सम्भ्रान्त अभिजात समझकर कम उम्रहोनेपर भी लोगोंने मुझे प्रधान बनानेका सुझाव दिया, छड़ीदार पण्डा नेमेरे नामकी घोषणा कर दी। छड़ीदार ने हम सबको हाव नदीमें अपनी-अपनी सुराही भरने काआदेश दिया। जलभरी सुराही लेकर हम लोग गड़ी हुई छड़ी के पास खड़े हुए। छड़ीदारने छड़ी का पूजन किया । गाँजा का भोग लगाकर दम लगायाऔर रक्तवर्ण आँखों से उसने छड़ी को उखाड़कर कन्धे पर रख लिया और हिङ्गलाज माता का जयघोष कर जब वह चल पड़ा तो जयध्वनि करते हुएहम सब लोग उसके पीछे-पीछे चल पड़े। हाव नदी को पार किया। बबूल,बेर और अन्य अपरिचित झाड़-झाड़ियों को नोचते चबाते दोनों ऊँट चल रहे थे। अपने-अपने ऊंट के बाजू में सटे हुए फरसा सँभाले दोनों ऊंटवाले चलरहे थे। उनके पीछे हम सब आतुरता और उत्कण्ठा समेटे चले जा रहे थे ।नीचे रेत ऊपर कांटेदार झाड़ियां, ऊँची-नीची जमीन, कभी टीले, टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता कांटोंसे भरा था। पग-पग पर कांटे चुभते थे, कहीं ऊँट आँखों से ओझल न हो जाएं, नहीं तो कण्टकाकीर्ण रेतीले मैदान में भटक भटककर यतीमों की तरह जिन्दगी से हाथ धो बैठें, इसलिए रुककर, बैठकर पैरों से कांटा निकालने में भी भय लग रहा था। रेगिस्तान में ऊँटही पथ-निदेशक होते हैं, ऊँट वाले नहीं । कहाँ जाना है, कौन-सा रास्ता है।
यह तो ऊँटवाले नहीं, ऊँट ही जानते हैं। हां, रात में यदि आसमान साफरहा तो ऊंटवाले सप्तर्षि और ध्रुवताराकी पहचान से पथदिशा पहचानते हैं, किंतु दिन में नहीं और ऊँट दिन हो या रात हो जहाँ उसे जाना है,जिधर पानी मिलने की सम्भावना रहती है, उधरका ही रास्ता वह पकड़ताहै । यदि उसके निर्देशन में ऊंटवाले या किसी अन्यने अपनी अक्ल भिड़ाईया छेड़-छाड़ की तो फिर ख़ुदा हाफिज़ ! जाना कहीं है और पहुँचे कहीं ।हो सकता है कि जहन्नुमके लिए टिकट मिल जाये ।
प्रायः सभी यात्रियोंको पहले से ही यह एहसास करा दिया जाता है.कि हिङ्गलाज की यात्रा यमद्वार की यात्रा से अधिक सङ्कटपूर्ण है, लेकिनकदाचित् उन्मादिनी जयावेन को इसका एहसास नहीं था, क्योंकि एक तो वह यौवन के उन्मादसे उन्मत्त थी, दूसरे पुत्रका मुख देखने के लिए अदम्यलालसा से वह भय ठुकराये हुए थी ।
बीस-बीस मनका भार लादे हुए दोनों ऊँट परमहंसकी भांतिअलमस्त चाल से चल रहे थे और बड़ी बेफिक्री से झाड़ियोंका चर्वण करतेहुए चल रहे थे। पौ फट रही थी, अंधेरा भाग रहा था और झाड़ियाँहिल-डुलकर 'टा-टा' करके हमसे विदा ले रही थीं। सूर्य की किरणों के साथ वालुकामय नीरस, निर्जीव धूल के समुद्र में हमारे पैर धँसने-फँसने और फिसलने लगे। ओह! मैंने अभी-अभी जिसे नीरस, निर्जीव समझा था,वह मेरे मनकी बात अन्तर्यामीकी भांति सुनकर प्रतप्त हो उठा है। पैर झुलसने लगे। उछल-उछलकर पैर रखने लगा। उछला तो पैर फिसला और मुंह के वल गिरकर धूल चाटने लगा। माता हिंगलाज ने कृपा की कि कन्धे पर लटकती हुई सुराही न ढुलकी, न टूटी और न छलकी जल्दी उठा और तुफान तथा गुलबदन का अनुचर वन दौड़ पड़ा, किंतु दौड़ कहाँ सका,रेत पैर पकड़कर पीछे की ओर घसीट लेती थी। आगे-पीछे दायें-बायें चांदी-सा चमकता हुआ रेगिस्तान और ऊपर से अग्नि-अभिषेक करता हुआ सूर्य जय माता हिङ्गलाज की ! कहाँ फँस गया घनचक्करमे। वापस भी तोनहीं जा सकता ?
हिमालय में मैंने हिम-नदियोंको पार किया, हिम-तूफानों को केलाकिंतु माता हिंगलाजके इस आग के दरियाने तो मुझे विपन्न बना डाला ।बान के ऊंचे टोलेपर चढ़ते ही दोनों ऊँट दिखाई पड़ गये । सुराही सँभाली और फिसलकर ढाल पार कर गया। गुलबदनकी परछाई पकड़े हुए चलनेलगा । कुछ दूर चलनेपर एक कृशकाय मोठे और ठण्डे जलकी नदी मिलगयो जो अमृतद्रव साबित हुई ।ऊंट बैठा दिये गये । सामान उतार लिया गया। कुछ लोग खानाबनाने की धुन में लकड़ियाँ ढूंढ़ने लगे, कुछ लोग हताश से लेट गये । मैं नदी में घुस गया। हाथ-मुँह धोया, भर-पेट पानी पिया । तृषा तो चली गयी किंतुताप न गया । कण्टकविद्ध शरीर नोचेसे कटिपर्यन्त जल रहा था । पानी मेंपड़े रहने से कुछ शान्ति मिली, बाहर निकला तो जीवराज भाईकी गोद में लेटी हुई उनकी नवोढ़ा पत्नी जल बिन मीन की तरह तड़प रही थी। उसकेजानु पर्यन्त पैर लहू-लुहान थे, साड़ी क्षत-विक्षत होकर उसकी देहयष्टि कोढाँकने में मजबूर हो गयी थी। लोगोंने सहारा दिया, जीवराज भाईने उसका मुख धोया, उसे जल पिलाया, वह कुछ चैतन्य होकर, कसम खाकर अपनेअंग ढांकने लगी ।
एक ऊंटवाला दोनों ऊँटोंको लेकर चराने चला गया। रेगिस्तान मेंलकड़ियां ढूंढना रत्न खोजना है, किंतु पेटकी ज्वाला सर्वोपरि होती है। लोगबिन-चुनकर जो लकड़ियां ले आये, वे समिधा के समान थीं। समस्या थी चल्हा कैसे बने। बालूकी दीवार कभी किसीने बनाई है ? ईंटा-पत्थर कानाम-निशान नहीं। लकड़ियाँ जलानेका प्रयास लोगोंने शुरू किया, वह सुलग रही थीं, किंतु जलनेका नाम नहीं लेती थीं। आटे की गोलियां गोले बना-बनाकर लोग उन्हें भूनते भानते रहे। कच्ची-पक्की रोटियां बनाईदाल-भात, शाकका मनसूबा मनमें ही रह गया। मेरे पास कुछ पकवानथे, मैंने उन्हें खाकर भरपेट नदी-जल पिया। हिङ्गलाज यात्रा का नियम है कि हर यात्री एक-एक रोटी ऊंटवालोंको दे और जहाँ कुआँ हो, वहाँ कुएँ केरखवाले को भी एक-एक रोटी देने का नियम है। उस रेगिस्तान में मीठे पानीका कुआँ एक नियामत है। दस-बीस कोसके इर्द-गिर्द कहीं कुआं हो तोयात्रियों का सौभाग्य समझे। लासबेला स्टेट का आदेश था कि जो आदमी जहाँ पर कुआं खोदे, उसकी वह रखवाली करता रहे। साथ ही दस-बीस कोस के इर्द-गिर्द जो घटना घटे, उसकी सूचना वह निकटवर्ती पुलिस चौकीको दे और उसका वेतन ? वेतनके नामपर एक रोटी। जो भी यात्री उधर सेगुजरें और वहाँ खाना बनायें तो एक रोटी कुऍके रखवाले को भी दें। यात्री न गये तो खुदा हाफ़िज़ ।अभी तो रोटी बनाने का हमारा प्रथम दिन ही था, कुआं तो मिलानहीं किन्तु कुएं के बारे में हम सब लोगोंको पहले से ही समझा दिया गया था, जिससे कुएँ के पहरेदारका हक न मारा जाए।
लोग खा-पी रहे थे, छड़ोदार चिलम में गांजा भरकर छड़ी भवानी कोभोग लगाकर दमपर दम लगा रहा था। आग्नेय नेत्रोंसे वह इधर-उधरदेखता तो मानो वैताल घूर रहा हो। छड़ी जहाँ गाड़ी हुई थी, उसकाउल्लङ्घन कोई नहीं कर सकता था। छड़ी हिङ्गलाज देवी की प्रतीक थी।
वह आगे-आगे चलती, उसके पीछे-पीछे चलना होता है। लोगोंने छड़ीदार को भी पेट भरने के लिए कुछ चाहिए-शायद यह अनुभव नहीं किया या ऊंटवालों, कुएंके रखवालोंकी तरह उसे रोटी देनेका नियम न हो किंतुथकी-हारी जयावेन छड़ीदारको न भूल सकी। उसने अपने हिस्से में से आधाछड़ीदारको दे दिया। छड़ीदार खुश हो गया और जीवराज भाई कुनमुना ने लगे। ऊंटवालोंको सब लोगोंने एक-एक टिक्कड़ निकाल कर दिया था।मेरे पास चना कुरमुरा था। मैने ऊंटवालेको दिया, शायद रोटीकी अपेक्षामेरा कुरमुरा मात्रामें अधिक रहा हो, इसलिए बुजुगं ऊंटवाला अपनीबलूची भाषामें मुझे बार-बार आशिष या धन्यवाद दे रहा था। ऊँट चरा-कर दूसरा कँटवाला भी आ गया। ऊंटोंको नदी के किनारे बैठाकर पानीपिलाया गया । वह एक घण्टे तक पानी पी-पीकर अपनी थैली भरते रहे।
शायद दो-तीन दिनके लिए उन्होंने पानीका स्टाक जमा कर लिया हो ।सामान ऊँटोंपर लादा जाने लगा। सब लोगोंने अपनी-अपनी सुराही में जन भर लिया। सूर्य अस्त हो रहे थे। क्षितिज रक्तवर्ण हो रहा था। धरतीने घूंघट काढ़ लिया था। उस समय वह क्षीणकाय नदीअसूर्यकी लोहित किरणोंसे सिन्दूरवर्ष हो गयी थी। ऐसा लगता था कि घूंघट ओढ़े हुए धरती की माँग में सिन्दूर-रेखा है।
सड़ीदारने हाँक लगाई। सब लोग छड़ी सामने खड़े हो गये। गाँजाका भोग धरकर छड़ीदारने कश खींचा। चिलम जल उठी, फिर सब लोगोने छड़ी को प्रणाम किया। छड़ीदारने छड़ीको उखाड़कर कन्धे पर रखाऔर जयमाता हिंगलाजका उच्चघोषकर वह चल पड़ा। उसके पीछे ऊँट और हम सब लोग चलकर नदी पार हुए।
आग का दरिया तारागण टिमटिमा रहे थे, चन्द्रमा का कुछ पता नहीं था। नीचेधूलका समुद्र, ऊपर अन्धकारमय असीम आकाश । अब ऊँट ही छड़ीदारबने हुए थे, आगे-आगे वह चल रहे थे और उनको घेरे हुए हम सब चलरहे थे। ऐसा लग रहा था कि शून्य आकाशमें हम लोग अन्तरिक्ष यात्री बने घूम रहे हैं। पशु, पक्षी, तरु, पल्लव, वीरुध सभी शून्य में विलीन होगये थे। दिनमें जो बालू आग बनी हुई थी वह शीतल स्वभावकी बनकरहमें दुलरा रही थी, पाँव पकड़कर जिद कर रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। हम एक पग आगे तो दो पग वह पीछे खींच लेती थी। हमें भयथा कि कहीं वालू के मोह में फँस गये तो दीन-दुनिया कही के नहीं रहेंगे।निस्तब्ध वातावरण में हिङ्गलाजकी जयका घोष जब निनादित होता था तब दिल काँप उठता था । मरे हुए मनसे कांपती आवाज से, हाँफते मुँह सेबड़ी मुश्किल से वह जय, पराजय बनकर निकल पाती थी ।
हमारे यात्री दलमें अधिकांश चायके गुलाम थे। चाय की चाह शायदहिङ्गलाज दर्शनकी चाहसे अधिक थी। एक ओर कहीं मद्धिम आग जलतीदेखकर कुछ लोग चायके लिए पागल हो उठे, किंतु बुजुर्ग कासिमने डपट दिया । सब शान्त हो गये। पता नहीं वह आग कैसी रही । दिन मेंरेगिस्तान में मृगतृष्णा आदमीको भटकाकर मार देती है और रात में शायदमरु भी कोई तृष्णा ही हो। कासिम मियां न जाने क्यों मुझपर मिहरवान हो गये । मेरे लड़खड़ाते हुए पैर, झुकता- फिसलता शरीर, सुराही को दो चारकरनेको उतारू हो गये तो उन्होंने मेरी सुराही स्वयं सम्भाल ली। उनका यह सहयोग, यह उपकार यात्राकी वापसी तक बरकार रहा ।
रात भर चलते रहे । रातके चौथे पहर एक जगह ऊँट रुक गये ।वहीं आसन बिछाकर लेटते ही नींद आ गयी। सुबह सूर्योदय के बाद फिरअनन्तकी ओर चल पड़े। प्रतप्त बालुकाकण, प्रचण्ड सूर्यातप दोनों हमें भून रहे थे।
इतने में •........... (शेष पुस्तक में द्रष्टव्य)
6) -जय हिङ्गलाज
हिंगलाज की मेरी यात्रा ‘आ बैल मुझे मार’ की तरह रही। तीनमहीना कश्मीर की सुखद सुषमाका रसपान करने के बाद शीतल-मन्द-सुगन्धपवन का स्पर्श प्राप्त करनेके बाद एकाएक अग्निकुण्ड में कूद पड़ा। यह मेरा बहशीपन ही था, क्योंकि मेरी कोई कामना नहीं थी। किसी कामना की पूर्तिके लिए देवी के दर्शनों के लिए कोई मनोती नहीं मान रखी थी और न धर्म-प्राण बनकर ही तीर्थ यात्रा के लिए पैर उठाये थे ।
नागनाथ के अखाड़े में कुल २७ यात्री एकत्र हो गये थे, उनमें एकस्त्री-पुरुषका जोड़ा भी था। पतिका नाम जीवराज करसनजी साँचोराथा और पत्नीका नाम जयावेन था । जीवराज भाईने तीसरी शादी कर जयावेनको पाया था । जयावेनकी उम्र २७ वर्षकी थी और जीवराज भाई की उम्र ५४ वर्षकी थी। दस वर्ष शादीको हो गये थे, किंतु जयावेन कीगोद नहीं भरी थी । सन्तान सुख प्राप्त करने, पुत्र का मुख देखने की मनौती मान रखी थी दोनोंने । कोई पुत्र-पुत्री न होनेपर हिंगलाज दर्शन के लिएआये थे ।
हम सत्ताईस तीर्थयात्रियों के अलावा एक छड़ीदार, दो ऊंटवाले सबमिलाकर तीस मानव प्राणी थे । ऊँटनी ‘गुलबदन’ और ऊँट ‘तूफान’ कोभी मिलाकर कुल ३२ प्राणी थे, जिनमें जयाबेन और गुलबदन दो स्त्रीलिंग शेष पुल्लिंग थे ।दोनों ऊँटोंपर सामान लाद दिया गया। तीसरे पहरके चार बजे थे,सब लोग अपनी-अपनी सुराही कन्धेपर लटकाकर ‘जय माता हिंगलाज’का उच्चघोष कर चल पड़े। कराची से बाहर निकलने पर खेत मिले, बंजरभूमि मिली, कुछ रेतीली, भुरभुरी जमीन मिली। झाड़ियां, भाड़, कांटे,कड़ मिले। बड़ा उत्साह था हम सब लोगों में । आषाढ़का महीना था ।बादल न बदली, न बूंद न लू-लपट । निरभ्र, निर्लिप्त आकाश। उछाह भरा वह वर्तमान बड़ा सुखद और सुनहला लग रहा था। भविष्य को कोई चिन्ता न थी । लगभग तीन-चार मील चलने के बाद कुश कण्टकाकीर्ण पथ मिला । कांटे चुभनेपर सी-सीकर आगे बढ़ते, दर्भ की नोक गड़ने परबल्लसे खून निकल पड़ता था, किंतु कोई हरकत नहीं, माता हिंगलाज कीजय बोलकर आगे बढ़ जाते । जयाबेनको गोद भर जानेका पक्का विश्वास था, इसलिए उसका उछाह हम सबसे छब्बीस दुगुन बावन था। वह तितली-की तरह फुदकती, बिजलीकी तरह चमकती, लह्रोंकी तरह इठलाती चलरही थी । झाड़ियाँ उसकी साड़ी पकड़कर जब रोक लेतीं तो वह ‘उई माँ’कहकर बैठ जाती और जीवराज भाई दौड़कर उसे झाड़ियोंके बाहुपाश सेमुक्त कराते । वह फिर फुदकती, उड़ती हुई आगे बढ़ती और कांटे चुभने पर हाय ! हाय ! कर लोट-पोट हो जाती तब तो कुछ क्षणोंके लिए सब लोगों को रुकना पड़ता था ।
उमङ्गों भरी राह चलते-चलते देखा सूर्य समुद्र में डुबकी लगा रहाहै। प्रकृति सान्ध्य परिधान धारण किये निशा की बाट जोह रही है।सूर्यास्त होते-होते हम लोग ‘हाव’ नदी के किनारे पहुँच गये । यही पहलापड़ाव था, उस यात्राका और वास्तविक तीर्थ-यात्रा यहीं से प्रारम्भ होती थी।
‘हाव’ नदी के इस पार सिन्ध प्रदेश की सीमा समाप्त होती है औरनदी पार करनेपर बलूचिस्तान के लासबेला राज्यकी सीमा प्रारम्भ होतीहै। लासवेला स्वाधीन राज्य था, उसी राज्य में देवी हिंगलाजकी अवस्थितिहै। बलूची हृष्ट-पुष्ट लम्बे-तड़ंगे शानदार जिस्म के घनी और स्वाभिमानीव्यक्तित्वके पानीदार व्यक्ति होते हैं। गुलबदन का मालिक शेरमुहम्मदसाढ़े ६ फुटका चालीस वर्षीय बाँका बल्लोच था और तूफान का मालिककासिम भीमकाय साठ वर्षीय पट्टा था। वह ‘साठा सो पाठा’ की कहावतचरितार्थ कर रहा था। दोनोंके हाथ में चमचमाते हुए फरसे थे। दोनों धीर,गम्भीर, मितभाषी और अतिशय विनम्र थे। अपनी-अपनी ऊँचाईके अनुसारवे चरित्र के भी ऊँचे थे ।ऊँटों से सामान उतार दिया गया । सबने अपनी-अपनी गठरी मुठरीअलग कर लो। मेरे पास बोरों और बोरियों में सुव्यवस्थित सामान इतना था कि उस सामान के कारण मैं सभी यात्रियों से समृद्ध और सम्पन्न बन गया था। यदि साधुवेला तीर्थ मुझे सम्पन्न न बनाता तो मैं ही सबसे निकृष्ट, मुफलिस मुसाफिर होता । चना चबाता, रोटी नसीब न होती और अगर चना समाप्त हो जाता तो वीरान रेगिस्तान में 'हुं फट् स्वाहा हो जाता।
छड़ीदार ने अपनी भाषा में कुछ पढ़कर छड़ी गाड़ दी, फिर गाँजा काभोग लगाकर चिलमको मुँह में सटाकर ऐसा कश खींचा कि चिलम आगउगलने लगी। हमारे पुरोहितजी के नेत्र आग्नेय हो गये। सब लोगोंने अपने-अपने ढङ्गका जल-पान किया, किसी ने चाय-चिवड़ा लिया, किसीने मोदकफोड़े, हमने मेवा खाया । प्रातः ३ बजेके लगभग कासिम और शेर मुहम्मद अपने-अपने ऊँटोंको उठ बैठ कराने लगे। छड़ीदारने हाँक लगाई। सब यात्री तैयार होगये । हाव नदी में स्नान किया। पण्डा सबके लिए एक-एक गेरुए रंगवस्त्र के टुकड़े हाथमें लिए था। हम सब उसको चारों ओरसे घेरकर खड़ेथे। उसने कड़कती आवाज में हम लोगों को यह शपथ दिलायी कि 'जबतक माता हिंगलाज के दर्शन कर पुनः यहाँ नहीं लौटेंगे, तबतक हम लोगसंन्यास धर्मके नियमों का पालन करेंगे। एक दूसरेकी यथाशक्ति सहायताकरेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, निन्दा के भाव हृदयमें नहीं रखेंगे, किंतु किसी भी हालत में अपनी सुराहीका पानी किसी दूसरे को नहीं देंगे, यहाँ तक कि पति-पत्नी को,पत्नी पतिको, पुत्र- पिताको, पिता-पुत्रको, मां-बेटेको, बेटा माँ को भी अपनी सुराहीका पानी नहीं देगा, जो इस नियमका उल्लंघन करेगा उसकी मृत्युनिश्चित होगी ।'
यह शपथ दिलाने के बाद उस तीर्थ पुरोहितने प्रत्येक यात्री के सिरपरगेरुए रङ्गके वस्त्र के टुकड़े बांध दिये, तदनन्तर यात्रियों में से एक आदमी कोप्रधान चुन लेनेका आह्वान किया। कदाचित् मेरे पास सबसे अधिक खाद्य-सामग्री होने के कारण मुझे विशिष्ट, सम्भ्रान्त अभिजात समझकर कम उम्रहोनेपर भी लोगोंने मुझे प्रधान बनानेका सुझाव दिया, छड़ीदार पण्डा नेमेरे नामकी घोषणा कर दी। छड़ीदार ने हम सबको हाव नदीमें अपनी-अपनी सुराही भरने काआदेश दिया। जलभरी सुराही लेकर हम लोग गड़ी हुई छड़ी के पास खड़े हुए। छड़ीदारने छड़ी का पूजन किया । गाँजा का भोग लगाकर दम लगायाऔर रक्तवर्ण आँखों से उसने छड़ी को उखाड़कर कन्धे पर रख लिया और हिङ्गलाज माता का जयघोष कर जब वह चल पड़ा तो जयध्वनि करते हुएहम सब लोग उसके पीछे-पीछे चल पड़े। हाव नदी को पार किया। बबूल,बेर और अन्य अपरिचित झाड़-झाड़ियों को नोचते चबाते दोनों ऊँट चल रहे थे। अपने-अपने ऊंट के बाजू में सटे हुए फरसा सँभाले दोनों ऊंटवाले चलरहे थे। उनके पीछे हम सब आतुरता और उत्कण्ठा समेटे चले जा रहे थे ।नीचे रेत ऊपर कांटेदार झाड़ियां, ऊँची-नीची जमीन, कभी टीले, टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता कांटोंसे भरा था। पग-पग पर कांटे चुभते थे, कहीं ऊँट आँखों से ओझल न हो जाएं, नहीं तो कण्टकाकीर्ण रेतीले मैदान में भटक भटककर यतीमों की तरह जिन्दगी से हाथ धो बैठें, इसलिए रुककर, बैठकर पैरों से कांटा निकालने में भी भय लग रहा था। रेगिस्तान में ऊँटही पथ-निदेशक होते हैं, ऊँट वाले नहीं । कहाँ जाना है, कौन-सा रास्ता है।
यह तो ऊँटवाले नहीं, ऊँट ही जानते हैं। हां, रात में यदि आसमान साफरहा तो ऊंटवाले सप्तर्षि और ध्रुवताराकी पहचान से पथदिशा पहचानते हैं, किंतु दिन में नहीं और ऊँट दिन हो या रात हो जहाँ उसे जाना है,जिधर पानी मिलने की सम्भावना रहती है, उधरका ही रास्ता वह पकड़ताहै । यदि उसके निर्देशन में ऊंटवाले या किसी अन्यने अपनी अक्ल भिड़ाईया छेड़-छाड़ की तो फिर ख़ुदा हाफिज़ ! जाना कहीं है और पहुँचे कहीं ।हो सकता है कि जहन्नुमके लिए टिकट मिल जाये ।
प्रायः सभी यात्रियोंको पहले से ही यह एहसास करा दिया जाता है.कि हिङ्गलाज की यात्रा यमद्वार की यात्रा से अधिक सङ्कटपूर्ण है, लेकिनकदाचित् उन्मादिनी जयावेन को इसका एहसास नहीं था, क्योंकि एक तो वह यौवन के उन्मादसे उन्मत्त थी, दूसरे पुत्रका मुख देखने के लिए अदम्यलालसा से वह भय ठुकराये हुए थी ।
बीस-बीस मनका भार लादे हुए दोनों ऊँट परमहंसकी भांतिअलमस्त चाल से चल रहे थे और बड़ी बेफिक्री से झाड़ियोंका चर्वण करतेहुए चल रहे थे। पौ फट रही थी, अंधेरा भाग रहा था और झाड़ियाँहिल-डुलकर 'टा-टा' करके हमसे विदा ले रही थीं। सूर्य की किरणों के साथ वालुकामय नीरस, निर्जीव धूल के समुद्र में हमारे पैर धँसने-फँसने और फिसलने लगे। ओह! मैंने अभी-अभी जिसे नीरस, निर्जीव समझा था,वह मेरे मनकी बात अन्तर्यामीकी भांति सुनकर प्रतप्त हो उठा है। पैर झुलसने लगे। उछल-उछलकर पैर रखने लगा। उछला तो पैर फिसला और मुंह के वल गिरकर धूल चाटने लगा। माता हिंगलाज ने कृपा की कि कन्धे पर लटकती हुई सुराही न ढुलकी, न टूटी और न छलकी जल्दी उठा और तुफान तथा गुलबदन का अनुचर वन दौड़ पड़ा, किंतु दौड़ कहाँ सका,रेत पैर पकड़कर पीछे की ओर घसीट लेती थी। आगे-पीछे दायें-बायें चांदी-सा चमकता हुआ रेगिस्तान और ऊपर से अग्नि-अभिषेक करता हुआ सूर्य जय माता हिङ्गलाज की ! कहाँ फँस गया घनचक्करमे। वापस भी तोनहीं जा सकता ? हिमालय में मैंने हिम-नदियोंको पार किया, हिम-तूफानों को केलाकिंतु माता हिंगलाजके इस आग के दरियाने तो मुझे विपन्न बना डाला ।बान के ऊंचे टोलेपर चढ़ते ही दोनों ऊँट दिखाई पड़ गये । सुराही सँभाली और फिसलकर ढाल पार कर गया। गुलबदनकी परछाई पकड़े हुए चलनेलगा । कुछ दूर चलनेपर एक कृशकाय मोठे और ठण्डे जलकी नदी मिलगयो जो अमृतद्रव साबित हुई ।ऊंट बैठा दिये गये । सामान उतार लिया गया। कुछ लोग खानाबनाने की धुन में लकड़ियाँ ढूंढ़ने लगे, कुछ लोग हताश से लेट गये । मैं नदी में घुस गया। हाथ-मुँह धोया, भर-पेट पानी पिया । तृषा तो चली गयी किंतुताप न गया । कण्टकविद्ध शरीर नोचेसे कटिपर्यन्त जल रहा था । पानी मेंपड़े रहने से कुछ शान्ति मिली, बाहर निकला तो जीवराज भाईकी गोद में लेटी हुई उनकी नवोढ़ा पत्नी जल बिन मीन की तरह तड़प रही थी। उसकेजानु पर्यन्त पैर लहू-लुहान थे, साड़ी क्षत-विक्षत होकर उसकी देहयष्टि कोढाँकने में मजबूर हो गयी थी। लोगोंने सहारा दिया, जीवराज भाईने उसका मुख धोया, उसे जल पिलाया, वह कुछ चैतन्य होकर, कसम खाकर अपनेअंग ढांकने लगी ।
एक ऊंटवाला दोनों ऊँटोंको लेकर चराने चला गया। रेगिस्तान मेंलकड़ियां ढूंढना रत्न खोजना है, किंतु पेटकी ज्वाला सर्वोपरि होती है। लोगबिन-चुनकर जो लकड़ियां ले आये, वे समिधा के समान थीं। समस्या थी चल्हा कैसे बने। बालूकी दीवार कभी किसीने बनाई है ? ईंटा-पत्थर कानाम-निशान नहीं। लकड़ियाँ जलानेका प्रयास लोगोंने शुरू किया, वह सुलग रही थीं, किंतु जलनेका नाम नहीं लेती थीं। आटे की गोलियां गोले बना-बनाकर लोग उन्हें भूनते भानते रहे। कच्ची-पक्की रोटियां बनाईदाल-भात, शाकका मनसूबा मनमें ही रह गया। मेरे पास कुछ पकवानथे, मैंने उन्हें खाकर भरपेट नदी-जल पिया। हिङ्गलाज यात्रा का नियम है कि हर यात्री एक-एक रोटी ऊंटवालोंको दे और जहाँ कुआँ हो, वहाँ कुएँ केरखवाले को भी एक-एक रोटी देने का नियम है। उस रेगिस्तान में मीठे पानीका कुआँ एक नियामत है। दस-बीस कोसके इर्द-गिर्द कहीं कुआं हो तोयात्रियों का सौभाग्य समझे। लासबेला स्टेट का आदेश था कि जो आदमी जहाँ पर कुआं खोदे, उसकी वह रखवाली करता रहे। साथ ही दस-बीस कोस के इर्द-गिर्द जो घटना घटे, उसकी सूचना वह निकटवर्ती पुलिस चौकीको दे और उसका वेतन ? वेतनके नामपर एक रोटी। जो भी यात्री उधर सेगुजरें और वहाँ खाना बनायें तो एक रोटी कुऍके रखवाले को भी दें। यात्री न गये तो खुदा हाफ़िज़ ।अभी तो रोटी बनाने का हमारा प्रथम दिन ही था, कुआं तो मिलानहीं किन्तु कुएं के बारे में हम सब लोगोंको पहले से ही समझा दिया गया था, जिससे कुएँ के पहरेदारका हक न मारा जाए।
लोग खा-पी रहे थे, छड़ोदार चिलम में गांजा भरकर छड़ी भवानी कोभोग लगाकर दमपर दम लगा रहा था। आग्नेय नेत्रोंसे वह इधर-उधरदेखता तो मानो वैताल घूर रहा हो। छड़ी जहाँ गाड़ी हुई थी, उसकाउल्लङ्घन कोई नहीं कर सकता था। छड़ी हिङ्गलाज देवी की प्रतीक थी।
वह आगे-आगे चलती, उसके पीछे-पीछे चलना होता है। लोगोंने छड़ीदार को भी पेट भरने के लिए कुछ चाहिए-शायद यह अनुभव नहीं किया या ऊंटवालों, कुएंके रखवालोंकी तरह उसे रोटी देनेका नियम न हो किंतुथकी-हारी जयावेन छड़ीदारको न भूल सकी। उसने अपने हिस्से में से आधाछड़ीदारको दे दिया। छड़ीदार खुश हो गया और जीवराज भाई कुनमुना ने लगे। ऊंटवालोंको सब लोगोंने एक-एक टिक्कड़ निकाल कर दिया था।मेरे पास चना कुरमुरा था। मैने ऊंटवालेको दिया, शायद रोटीकी अपेक्षामेरा कुरमुरा मात्रामें अधिक रहा हो, इसलिए बुजुगं ऊंटवाला अपनीबलूची भाषामें मुझे बार-बार आशिष या धन्यवाद दे रहा था। ऊँट चरा-कर दूसरा कँटवाला भी आ गया। ऊंटोंको नदी के किनारे बैठाकर पानीपिलाया गया । वह एक घण्टे तक पानी पी-पीकर अपनी थैली भरते रहे।
शायद दो-तीन दिनके लिए उन्होंने पानीका स्टाक जमा कर लिया हो ।सामान ऊँटोंपर लादा जाने लगा। सब लोगोंने अपनी-अपनी सुराही में जन भर लिया। सूर्य अस्त हो रहे थे। क्षितिज रक्तवर्ण हो रहा था। धरतीने घूंघट काढ़ लिया था। उस समय वह क्षीणकाय नदीअसूर्यकी लोहित किरणोंसे सिन्दूरवर्ष हो गयी थी। ऐसा लगता था कि घूंघट ओढ़े हुए धरती की माँग में सिन्दूर-रेखा है। सड़ीदारने हाँक लगाई। सब लोग छड़ी सामने खड़े हो गये।
गाँजाका भोग धरकर छड़ीदारने कश खींचा। चिलम जल उठी, फिर सब लोगोने छड़ी को प्रणाम किया। छड़ीदारने छड़ीको उखाड़कर कन्धे पर रखाऔर जयमाता हिंगलाजका उच्चघोषकर वह चल पड़ा। उसके पीछे ऊँट और हम सब लोग चलकर नदी पार हुए।
आग का दरिया तारागण टिमटिमा रहे थे, चन्द्रमा का कुछ पता नहीं था। नीचेधूलका समुद्र, ऊपर अन्धकारमय असीम आकाश । अब ऊँट ही छड़ीदारबने हुए थे, आगे-आगे वह चल रहे थे और उनको घेरे हुए हम सब चलरहे थे। ऐसा लग रहा था कि शून्य आकाशमें हम लोग अन्तरिक्ष यात्री बने घूम रहे हैं। पशु, पक्षी, तरु, पल्लव, वीरुध सभी शून्य में विलीन होगये थे। दिनमें जो बालू आग बनी हुई थी वह शीतल स्वभावकी बनकरहमें दुलरा रही थी, पाँव पकड़कर जिद कर रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी। हम एक पग आगे तो दो पग वह पीछे खींच लेती थी। हमें भयथा कि कहीं वालू के मोह में फँस गये तो दीन-दुनिया कही के नहीं रहेंगे।निस्तब्ध वातावरण में हिङ्गलाजकी जयका घोष जब निनादित होता था तब दिल काँप उठता था । मरे हुए मनसे कांपती आवाज से, हाँफते मुँह सेबड़ी मुश्किल से वह जय, पराजय बनकर निकल पाती थी ।
हमारे यात्री दलमें अधिकांश चायके गुलाम थे। चाय की चाह शायदहिङ्गलाज दर्शनकी चाहसे अधिक थी। एक ओर कहीं मद्धिम आग जलतीदेखकर कुछ लोग चायके लिए पागल हो उठे, किंतु बुजुर्ग कासिमने डपट दिया । सब शान्त हो गये। पता नहीं वह आग कैसी रही । दिन मेंरेगिस्तान में मृगतृष्णा आदमीको भटकाकर मार देती है और रात में शायदमरु भी कोई तृष्णा ही हो। कासिम मियां न जाने क्यों मुझपर मिहरवान हो गये । मेरे लड़खड़ाते हुए पैर, झुकता- फिसलता शरीर, सुराही को दो चारकरनेको उतारू हो गये तो उन्होंने मेरी सुराही स्वयं सम्भाल ली। उनका यह सहयोग, यह उपकार यात्राकी वापसी तक बरकार रहा ।
रात भर चलते रहे । रातके चौथे पहर एक जगह ऊँट रुक गये ।वहीं आसन बिछाकर लेटते ही नींद आ गयी। सुबह सूर्योदय के बाद फिरअनन्तकी ओर चल पड़े। प्रतप्त बालुकाकण, प्रचण्ड सूर्यातप दोनों हमें भून रहे थे।
7) ••••••हिममानव से भेंट•••••
भूल न सकूँगा कभी अपने उस यायावर जीवन को । जब न मरने का भय था और न जीने की लालसा।कामना सिर्फ यही रहती कि चलता रहूँ, घूमता रहूँ, नित्य नवीनता का अनुभव करता रहूँ और अपने देश की प्रकृति की विचित्रता, विविधता की जानकारी प्राप्त करूँ।
मेरी इस कामना को तीव्रतर बनाने में, मेरी इच्छाओं को प्रज्वलित करने में ईंधन का काम दिया डाॅक्टर स्वामी शान्तानन्द सरस्वती महाराज ने | वह विद्वान् संन्यासी जितना विद्वान् उससे अधिक त्यागी और सर्वाधिक मस्त था। मैं कह नहीं सकता कि उनके मिल जाने से मेरी पूर्णता हुई या मेरे मिल जाने से उनकी कमी पूरी हुई। कुछ भी हो हम दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए थे ।
मुझे वे मिले थे कश्मीर की शङ्कराचार्य पहाड़ी में । मेरी वह कश्मीर यात्रा तीसरी और अन्तिम थी, स्वामी जी ने मुझे उकसाया अमरनाथ चलने के लिये जब कि अभी अमरनाथ यात्रा का समय नहीं था ।
हम दोनों चल पड़े। दोनों के पास सीमित साधन थे । एक मानी में हम सब साधनहीन थे ।अमरनाथ गुफा जाने के लिये हम लोग पहलगाम तक तो ठीक रास्ते से गये किन्तु वहाँ से 'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः' वाली कहावत चरितार्थ हुई। बर्फीले पहाड़ों और घने जंगलों से होकर चलता, जीवन का, प्रकृति का और विपत्तियों का अनुभव प्राप्त करना ही शायद हमलोगों का अभीष्ट था। स्वामी जी प्रयोगवादी स्वभाव के थे। जीवन की नन्हीं-मुन्नी बातों में, कार्यों में वे नये प्रयोग करने में अभ्यस्त थे। उनके प्रयोगवाद ने मुझे भी चक्कर में फँसा दिया ।
जो कुछ कपड़े पहने हुए थे उनके अलावा एक कम्बल एक डंडा और पैर में जूते छोड़कर और कुछ भी हमारे पास न था । जहाँ कहीं फल, फूल मिल जाते खा लिया करते थे। स्वामीजी कंद-मूल के पारखी थे-जहाँ तक कंद-मूल मिलते वे हर हिकमत से उखाड़ कर ले आते और दोनों कच्चा चबा जाते । हम हिमाच्छादित पर्वतमाला के कहीं चरणों के नीचे चलते कभी उनकी कटि पर, कभी पीठ पर और कहीं हमें उनके शिखर पर चढ़ना पड़ जाता था ।
वनस्पति बहुत कम मिलती, पशु-पक्षी भी बहुत कम दिखाई पड़ते। हम बिना किसी दिशा ज्ञान के चलते, जहाँ थक जाते वहीं दुबक कर सो जाते। कई मौके तो ऐसे भी आये कि जाड़े के मारे आइसक्रीम बन गए ।
हम दोनों ने यह समझ लिया कि अमरनाथ के दर्शन तो अब मिलेंगे नहीं किन्तु उस भूमि के दर्शन हम कर रहे थे, जहाँ शायद कोई जाता नहीं। दो दिन से कुछ भी खाने को न मिला, पानी भी जहाँ कहीं मिलता वह मानो हिमप्रलय की प्रतीक्षा करता हो । तीसरे दिन हमें एक घाटी मिली वहाँ वनस्पति भी यत्र-तत्र दिखाई पड़ी, चिड़ियाँ भी उड़ती हुई नजर आईं। एक झरना मिला जिसके आस-पास एक ऐसी हरी-हरी लता बौड़ी हुई थी जिसमें मकोइया की तरह लाल-लाल पके हुए सुन्दर फल गुच्छे के गुच्छे लदे हुए थे ।
स्वामीजी ने कहा कि कुदरत ने खाने के लिये फल तो दिया, भले ही यह जहर हो । अब तो इसे खाना ही चाहिए। हम दोनों फलों को तोड़ने लगे। मैं खाने जा रहा था कि स्वामी जी ने रोक कर कहा, पहले मुझे खाने दो पता नहीं कैसा फल है-उन्होंने दस बीस फल एक साथ मुख में रखकर बताया बहुत मीठे और स्वादिष्ट फल हैं-यह बात दूसरी है कि इस मधुरता में विष छिपा हो । मैंने कहा स्वामीजी मुझे तो खाने दीजिये, मरेंगे तो साथ ही मरें।
यदि बिना खाये मैं जीवित रह गया तो अकेले तड़प-तड़प कर मरने से बेहतर है कि हम दोनों एक-दूसरे को देखते हुए मरें। हम दोनों ने भर पेट फल खाया, झरने का पानी पिया और जेब में जितने फल भरे जा सकते हैं उतने तोड़ कर भर लिये। आगे चलने पर एक गुफा मिली जिसके द्वार पर जटा खोले हुए एक महात्मा मिले। कई दिन बाद मनुष्य जाति को देखकर हमारी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह महात्मा हमारी भाषा से सर्वथा अपरिचित थे, हम कुछ कहते तो वे अपनी भाषा में कुछ और कहते। स्वामी शान्तानन्द तिब्बती, लद्दाखी भाषाओं से परिचित रहे, वे उनसे रुक-रुक कर उनकी भाषा में बोलने लगे ।
उस परिचय से हमें यह मालूम हुआ कि हम अमरनाथ के बजाय लद्दाख की ओर जा रहे हैं। और जो दिशा या कुमार्ग अपनाया है, उससे इस जन्म में पहुँच ही नहीं सकते ।
उन महात्मा जी के बतलाने पर हम दोनों वहाँ से ५ मील दूर एक नाला देखने गए। सुबह के चले शाम को पहुँचे। उस नाले का नाम महात्मा जी ने 'सीताझ्योरी' बतलाया, उसकी विशेषता यह रही कि दुनियाँ की किसी भाषा में यह कहा जाय कि 'सीताजी रामजी आए' तो नाले का प्रवाह कुछ तेज हो जाता था और बीच में यदि यह कह दिया जाय कि रावण आया है तो प्रवाह मध्यम हो जाता था। स्वामी शान्तानन्दजी जितनी भाषायें जानते थे सबका उपयोग उस समय उन्होंने किया था— उस नाले का विज्ञान आज तक किसी की समझ में न आया ।
रात हो जाने से न तो हम आगे जा सकते थे और न पीछे लौट सकते थे, इसलिए उसी नाले का पानी पीकर हमने एक शिला में मुँह छिपाकर रात बितायी ।
सबेरे उठकर चलने को हुए कि हम दोनों जहाँ बैठे थे वहीं इस प्रकार अकड़े हुए बैठे रहे मानों किसी ने हमें गाड़ दिया है।
दोपहर तक अकड़े बैठे रहने के बाद जब धूप लगी तब कहीं हम सीधे हो पाये।
वहाँ से चलने को हुए तो दिग्भ्रम हो गया, हम वस्तुतः आगे जाना चाहते थे किन्तु अज्ञान से पीछे लौट पड़े किन्तु पहले के मार्ग से नहीं। हम पहाड़ों की छोटी-मोटी ऊँचाई नापते धीरे-धीरे चढ़ते-उतरते चल रहे थे कि अचानक यती -यती की पुकार हमें सुनाई पड़ी-हम भयभीत होकर इधर-उधर देखने लगे, तो अकस्मात् हमारी दृष्टि एक हिमाच्छादित पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो १० फुट से कम लम्बा न होगा, सारा शरीर नंगा किन्तु बड़े-बड़े बालों से ढका हुआ था - और उसका त्रिभुजाकार शिर बड़ा भयावना था—वह वनमानुष शायद हमारे पास से ही गुजरा था किन्तु उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह गया छूमन्तर हो गया । हमने जब होश संभाला तो देखा कि बर्फ पर उसके पैरों के निशान बने हुए थे। उसके पैर की पाँचों अंगुलियाँ बर्फ पर साफ उपटी हुई थीं।
हमने समझा यह मनुष्य नहीं राक्षस होगा, जैसा कि पुराणों में राक्षसों के रूप, गुण, कर्म के वर्णन मिलते हैं, वही उसके भी रहे। मनुष्य और पशु की कौन कहे चिड़ियाँ भी उड़कर इतनी तेजी से पर्वत शिखर पर नहीं जा सकती । वह तो अग्निबाण बनकर छूमन्तर हो गया था।
सचमुच हम अधिक भयत्रस्त हो चुके थे। चुपचाप खड़े काँप रहे थे। थोड़ी देर में स्वामी जी ने पूॅंछा कि यती- यती की आवाज किसने दी है। हम सोच रहे थे कि कोई अदृश्य शक्ति ने हमारे बचाव के लिये यह ध्वनि की होगी, कि इतने में ढाल पर से वही महात्मा आते हुए हमें दिखाई पड़े तो हम चिल्ला उठे ।
उन्होंने दूर से ही हमें आश्वासन दिया - कुछ देर बाद वह हमारे पास आये तो उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि नरभक्षी यती के ग्रास बनने से हम लोग बच गये। स्वामीजी ने पूॅंछा कि यती क्या है तो उन्होंने बताया कि बर्फ के पहाड़ों का यह नरभक्षी मानव है । इसमें अपार शक्ति और साहस रहता है। मनुष्य,पशु जो भी इसके हाथ लगता है झपट कर उठा भागता है। वायु की भाॅंति इसकी गति अबाध है, यह अजेय प्राणी है।
यह सब सुनकर हमारा सारा जुनून शान्त हो गया, हम श्रीनगर लौटने के लिये उतावले हो गये। महात्मा जी के साथ चल कर शाम को उनकी गुफा में पहुँच कर रात में वहीं विश्राम किया । सवेरे महात्मा ने हमें दिशा का बोध कराया और किसी पेड़ या लता की पतली-पतली दो जड़े देकर कहा कि इसमें से एक की एक अंगुल जड़ खा लेने से भूख-प्यास तीन दिन तक न लगेगी और दूसरी की एक अंगुल जड़ खा लेने से भूख प्यास खुल जाएगी। हमने भूख प्यास न लगने वाली जड़ वहीं खायी और प्रस्थान किया । सत्रह दिन बाद श्रीनगर लौटने पर दूसरी जड़ी जब खायी तो भूख प्यास खुल गई । श्रीनगर,आने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमने हिममानव से मुलाकात की थी।
******
स्मृति के हस्ताक्षर
पण्डित देवदत्त शास्त्री
Pandit Devdutt Shastri did very important research on three levels-
1). Various important places of Himalayas.
2). Various languages.
3). Medical system of Vedic science.
Firstly, by going to Himalayas, he described Vedni (place of origin of Vedic hymns), Kuber ki Alka (Yakshanagari described in Meghdoot), Satopath (the story of the demise of Yudhishthira etc. in Mahabharata), etc. Secondly, through Sanskrit grammar, in collaboration with Miss Crowne, head of Academy of Oriental Languages, he deciphered the extinct languages of the world, in which the deciphering of Injo language was unique. Thirdly, by completely classifying the mantras of Atharvaveda, establishing mantra therapy as divine therapy with evidence, he established Atharvan therapy, which, after testing it experimentally, cured lakhs of people of the world. Following are some examples of various research and formulas of Pandit Devdutt Shastri Ji-
1) - "-ऋचाओं की जन्मभूमि वेदनी-
छिपलाकेदार से लौट कर हम कसौनी आए । यहाँ आते ही शान्तानन्द ने मुझे वेदनी का भूगोल बतलाते हुए कहा कि क्षीर स्वामी, तुम वेदनी जाओ । वह स्थान परम पुनीत अत्यन्त रमणीक है । ऋषियों ने वैदिक ऋचाओं का साक्षात्कार वहीं किया था । इतना बतलाकर वह यह कहकर चले गए कि हम तुम्हें मिल जाएँगे । शान्तानन्द जी के स्वभाव और प्रकृति से मैं परिचित था, यह भी विश्वास था कि मुझे जहाँ कहीं भेजेंगे उसमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर होगा,और अचानक उनके गुम हो जाने का कोई महान् रहस्य अवश्य होगा, इसलिए मैंने कभी भी साथ चलने का आग्रह उनसे नहीं किया और न अकेले जाने में किसी प्रकार का भय किया था ।
कसौनी ऐसा सुरम्य स्थल है, जहाँ से हिमालय का विस्तार और उस का गौरव देखा जा सकता है । कसौनी से गरुड़ तक केवल उतराई ही उतराई है । कसौनी से गरुड़ जाने के लिए सोमेश्वर घाटी से जाना पड़ता है । यह घाटी क्या बनात का एक टुकड़ा है । सारी धरती लहलहाते धान के खेतों और मुस्कुराते हुए फूलों से भरी पड़ी है । प्रकृति यहाँ नृत्य करती हुई - सी प्रतीत होती है । गरुड़ से ग्वालदम तक कठिन चढ़ाई पार करने के बाद चीड़ और देवदारु के घने जंगल मिलते हैं, बीच - बीच छोटे - छोटे गाँव और डाक बँगले भी मिलते है । अखरोट, सेव, नाशपाती बहुतायत से है । यहाँ से नन्दा,घुंघटी और त्रिशूल के शिखरों कि चमक दमक देखने को मिलती है । एक नदी जिसे पिंडर कहते है, उसका किनारा पकड़कर मैं चल रहा था । मुझे भेड़ चराने वाले गड़रियों से पता चला कि इस जंगल में चीड़ का एक वृक्ष संसार का सबसे ऊँचा वृक्ष है और देवदारु का एक वृक्ष हजारों वर्ष पुराना है । आगे चलने पर पिंडर और कैल नदी का किनारा पकड़कर चलते हुए मैंने एक दर्रा पार किया तो विस्तृत चौरस मैदान मिला । अद्द्भूत, अपूर्व दृश्य था वहाँ का । हिमालय कि सम्पूर्ण सुषमा सिमटकर वहीं आ गई थी ।
हिमालय नाम ही व्यक्त करता है कि इस नाम से पर्वत की चोटियाँ सतत् हिमाच्छादित रहती है । हिमाच्छादित शिखर - श्रेणियों को सतत् हिमाच्छादित हिमालय कहा जाता है, जहाँ पर वर्ष भर हिमपात होता रहता है और पर्वत चोटियाँ सतत हिममण्डित रहती है । जहाँ पर वर्ष के कुछ ही महीनों तक हिम रहता है, उसे उपहिमालय कहते है । और जो गिरिशृंगो का निचला भाग है, जहाँ बर्फ नहीं जमा करती है, उसे हिमालय कि तराई कहते है । सतत - हिमाच्छादित हिमालय की दक्षिणी सीमा पर कूर्मांचल की पर्वतमाला है, जो तिब्बत और भारत को अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा है । सतत हिमाच्छादित हिमालय तिब्बत की पसली तक अड़ा हुआ है । कैलास, मानसरोवर राक्षसताल आदि सतत हिमालय के शिरोभाग मैं स्थित है । सतत हिमाच्छादित हिमालय पश्चिम में बन्दर पूँछ, स्वर्गारोहण शिखर से लेकर नेपाल तक चला जाता है । इस हिमालय शिखर श्रेणी के अंतर्गत सतोपथ, चतुःस्तभ्, नन्दा देवी, नन्दा कोटा, पंचचूली आदि श्रेणियाँ है, जो नेपाल के उत्तर पूर्व तक चली जाती है । सतत हिमाच्छादित हिमालय की पर्वत श्रेणियों के दर्शन से जो आनन्द प्राप्त होता है, वह अनिर्वचनीय है, उसे व्यक्त करने में भाषा का सम्बल निर्बल पड़ जाता है । सूर्योदय और सूर्यास्त से समय इन हिमखंडित शिखरों का रंग, रूप और दिव्य सौन्दर्य देखते हि बनता है । वेदों में ऋषियों ने जो उषस् गीत और सूर्योदय गान गाए है; उनकी अनुभूति, उनका साक्षात्कार यहीं होता है ।
वेदों में प्रकृति का सौन्दर्य - वर्णन विश्व साहित्य में अद्वितीय माना जाता है , किन्तु प्रत्यक्ष देखने पर तो वैदिक ऋषियों के प्राकृतिक वर्णन भी मुझे फीके लगे । अतिशयोक्ति न समझी जाए तो मैं यह कहने की धृष्टता करना चाहता हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमाच्छादित हिमालय के शिखर जो रंग रूप धारण करते है, उन्हें देखकर देखने वाले समाधिस्थ हो जाते है । मैंने कोणार्क का सूर्योदय और कन्याकुमारी का सूर्यास्त भी देखा है, निश्चय ही विश्व में ये अद्वितीय है, किन्तु हिमालय के हिमाच्छादित शिखरों के सूर्योदय और सूर्यास्त भूगोल के नहीं दिव्यलोक के हैं। उनकी तुलना के सभी सौन्दर्य से नहीं कि जा सकती है ।
वेदनी के प्राकृतिक सौन्दर्य ने तो मुझे पागल बना दिया था और वहाँ के सूर्योदय ने तो मुझे इतना विमुग्ध, विमोहित किया मैं बेसुध होकर घंटों तक जड़वत खड़ा रह गया था । वेदनी वह भूमि है, जहाँ पर वेदों कि ऋचाओं का साक्षात्कार ऋषियों, मुनियों ने किया था, अथवा वेदों कि शाखाओं कि रचना की होगी । हिमालय पर्वत अनेक पर्वतों, गिरिशिखरों के समुच्चय का नाम है । पर्वतमालाएँ और गिरी - शिखर सब मिलकर हिमालय पर्वत नामरूप धारण करते है । हिमालय का अन्त:भाग अथवा हिमाच्छादित हिमालय गिरी श्रृंगो का मुकुट धारण कर बड़े ऐश्वर्य और गर्व से स्थित है । दर्शनार्थी या पर्यटक एक के बाद एक शिखर को पार करता हुआ हिमालय के विभिन्न रूपों के दर्शन करता हैं ।मैदान और पठार बहुत कम, सीमित और नाममात्र के लिए मिलते है अथवा यह समझें कि मैंने अपने भ्रमण - काल में केवल गिरी श्रृंगो को ही देखा है, किन्तु समुद्रतल से १२ हजार फ़ीट की ऊँचाई पर सतत हिमाच्छादित हिमालय के वक्ष पर स्थित बिस्तोला बेदनी और आली जैसे ओर - छोर रहित घास के मैदान को देखकर मेरी आँखे फटी कि फटी रह गई । हिमालय के ये विशाल पठार प्रकृति कि अद्भुत शिल्प - सर्जना है ।
त्रिशूल ओर नन्दा घुंघटी गिरिमालाओं को पार करने के बाद मुझे ये दूर्वा भू - खंड को देखने को मिले । सौन्दर्य की अनेकानेक कल्पनाएँ की जा सकती हैं, प्राकृतिक वैभव के अनेक वर्णन किए जा सकते है, किन्तु सच कहता हूँ, वेदनी पहुंच कर कवि की सारी कल्पनाएँ कुण्ठित हो जाएँगी । रूपदक्ष मनुष्य की वाणी, लेखनी और तूलिका में इतनी शक्ति कहाँ कि वह इस दिव्यधाराधाम का वर्णन या चित्रण कर सके । वेदनी को भूस्वर्ग कहूँ या हिरण्मय लोक अथवा देवांगनाओं की क्रीड़ा भूमि या प्रकृति का अद्वितीय शिल्प ।
प्रकृति का अक्षुष्ण - रूप महोत्सव मुझे यहीं वेदनी में देखने को मिला । केवल आँखे ही नहीं, बल्कि मेरे रोम - रोम के रन्ध्र उस सौन्दर्य का उपभोग कर रहे थे। यहाँ आकर मनुष्य को अपनी लघुता का बोध होता है । यहीं आकर मधुर वाणी मौन हो जाती है, यहीं आकर कल्पनाएँ जड़ हो जाती है और यहीं आकर प्रकृति और परमात्मा के विराट रूप के दर्शन होते हैं ।
हिमालय का उदात्त सौन्दर्य वेदनी से ही देखा और भोगा जा सकता है । प्रातः काल तथा मध्याह्न में जब सूर्य का प्रकाश फैलता है तब त्रिशूल, नन्दा घुंघटी, चतुःस्तभ्भ, बदरीनाथ, केदारनाथ की सुवर्णमयी, रजतमयी दमकती हुई चोटियाँ दर्शक को पागल बना देती है । यह मनोमोहक उन्मद दृश्य धरती और आकाश का भेद, जीवन और जहान का भेद, जिन्दगी और मौत का भेद मिटाकर मनुष्य को द्वन्द्वातीत बना देता है, मीलों फैले हुए वेदनी के मैदान में हरी - हरी दूब ही दूब है । खोजने पर कहीं एक कंकड़ी, कंकड़, पत्थर नहीं मिलता है । उस दिन आकाश स्वच्छ था । वेदनी की धरती हरित परिधान पहने हुए अद्भुत मोहकता, अपूर्व सुंदरता धारण किए हुए थी । हरी - हरी दूब इतनी मुलायम, इतनी सुन्दर कि ईरानी गलीचा भी उसके आगे मात था । दुर्बादल के गुदगुदे गलीचे पर चलता हुआ मैं एक ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ हरी - हरीतिमा के बीच फूलों का उद्यान था । वह प्राकृतिक उद्यान था । उस उद्यान के बीच एक शुभ्र मानसरोवर था । उसका जल स्फटिक की तरह पारदर्शक था । तरह - तरह की मछलियाँ उसमें तैर रही थीं । सरोवर की तरंगे वैदिक ऋचाओं की भाँति संश्लिष्ट थीं । धीर समीर बह रहा था । मन्द - मन्द पवन से कोमल गान्धर स्वर मुखरित हो रहा था । मैं विमुग्ध विमोहित बना घंटों सरोवर के इधर - उधर टहलता रहा, उसको देखता रहा, उसको स्पर्श करता था और उसके जल से मार्जन तथा आचमन करता था । एक शुद्ध मनोरम परिसर में बैठ गया । मन निश्चल और प्रशान्त था । नयन खुले हुए थे । हृदय में अलौकिक आस्था का भाव जाग्रत था । इसी समय मुझे वैदिक ऋचाओं की मन्द - मन्द मधुर गूँज सुनाई पड़ी । मैं इधर - उधर देखने लगा कहीं कोई नहीं किन्तु वैदिक ऋचाओं की गुंजार सुनाई पड़ रही थीं । वेदनी की भूमि में मुझे एक भी कीट पतंग नजर न आया । हाँ, सरोवर के आस - पास बैठे हुए, उड़ते हुए सुन्दर पक्षी अवश्य थे । वैदिक ऋचाओं की अबाध गुंजार ने मुझे भ्रम में डाल दिया था । मैं ऋचा - गान की दिशा खोजने के लिए उठ खड़ा हुआ । जिधर जाता उधर ही गुंजन किन्तु दिखता कुछ भी नहीं था । न कोई गुफा थीं वहाँ, न कोई कुटीर । फिर वे ऋचा - गान के स्वर कहाँ से मुखरित हो रहे है । बहुत घूमा, किन्तु कुछ दिखाई न पड़ा तब सहसा मेरे हृदय में ' ऋृचोsक्षरे परमो व्योमन ' यह ऋचा उदबुद्ध हुई । मुझे समाधान मिल गया की वैदिक ऋचाएँ आकाश में निरन्तर गूँजा करती हैं । निश्चय ही ऋषियों ने यहीं पर ऋचाओं का साक्षात्कार किया होगा ।
निश्चिन्त होकर मैंने सोचा की वेदनी की मेदनी कहाँ तक फैली है -- पता लगाया जाए । लगभग ६ मील चलने के बाद उस वेदनी भू का अन्तिम छोर मील गया और त्रिशूल शिखर के एक भाग में कदाचित आवागमन के लिए प्रकृति निर्मित एक दर्रा मिला मैं उसी में समा गया । दर्रा पारकर मैं चलता रहा । चलते - चलते एक पर्वत पर हिमाच्छादित सरोवर मिला । तट पर पहुंचने के साथ ही अँधेरा हो गया तो मैंने वहीं रात बीतने का निश्चय कर अपना दंड कमण्डल रख दिया ।
त्रिशूल गिरी शृंग के नीचे पर्वत के एक सीधे ढलान पर स्थित उस झील के किनारे मैं बैठा था । साँय साँय करती हुई हवाएँ चल रही थीं । उग्रशीत से मैं उकडू - मुकड़ू हो रहा था, झील का जमा हुआ पानी चकम उठता था । भूल न सकूँगा वह रात । संध्या अलसाकर क्षितिज की नीली चादर ओढ़कर सो गई थी और निशा प्रकृति के वक्ष पर चौक पूर रही थी । पश्चिम की ओर लाल, गुलाबी केसरिया रंग के छोटे - छोटे बादल करि - शावक से लग रहे थे । चन्द्रमा मंद गति से क्षितीज की चढ़ाई चढ़ रहा था । ऊपर - नीचे; दाएँ - बाएँ चारों ओर कुहरे का समुद्र उमडने लग गया था । नाजुक रेशमी रंग का झीन - सा कुहरा नन्हे बच्चे की घुंघराली अलकों की भांति जान पड़ता था ।
जाड़े से ठिठुरता हुआ भी झील का वह प्राकृतिक नैश्य सौन्दर्य देखकर मनोमयूर नाच उठा । उस निर्जन किन्तु मनोरम झील के तट पर सुन्दर सपनों का मेला लग गया था । कुहरे की झीनी आसमानी मशहरी के अन्दर सोइ हुई वन - श्री के निद्रित लावण्य के अस्फुट दर्शन से मैं विमुग्ध बन रहा था । रात घिर आई थी । आसमान दष्टि पथ पर नहीं आ रहा था, उस पर काले, ऊदे रंग के बादल रेंग रहे थे । ऐसे अनुपम वातावरण में फैली हुई प्राकृतिक सुषमा ने मुझे वशीभूत कर लिया था । मन्त्र कीलित - सा ' न ययौ न तस्थौ ' की स्थिति का अनुभव कर रहा था । बड़ा विचित्र ऐन्द्रजालित सम्मोहन था ।
अपनी कमरी से तन बदन को ढाँके उस घनी रात में अकेला मैं जीवन - मरण के मोह ओर भय से विमुक्त अपलक नेत्रों से छवि का पान कर रहा था । भौतिकता से विरक्त प्रकृति के सजीले सौन्दर्य से अनुरक्त होकर मैं उठ खड़ा हुआ, कुछ दूर चलकर फिर बैठ गया और अज्ञात, अचिन्तन में मग्न हो गया कि सहसा दर्द भरी बाँसुरी कि तान सुनाई पड़ी । दिल तड़प उठा।दर्द भरी बाँसुरी कि ध्वनि क्रमशः बढ़ती हुई सारे वातावरण में व्याप्त हो गई तो लय - ताल से बजते हुए घुंघुरुओं कि ध्वनि सुन कर मैं चहक उठा । बाँसुरी की धुन मेरे ह्रदय में पीड़ा भर रही थी और घुंघुरुओं की रुन - झुन झनकार मुझे उन्मद बना रही थी । विचित्र सितासित का संगम बन रहा था मेरा हृदय ।
कठोरशीत, बर्फानी हवा के थपेड़े भूल कर रात भर मैं बाँसुरी की तान और घुंघुरुओं की रुनझुन सुनता हुआ एक ही स्थान पर जड़ बन कर स्थिर रहा । न नींद थी, न भय था, न कल्पना थी, न शीत था, न वात था और न कोई जिज्ञासा ही थी । थी तो केवल एक उन्माद भरी सिहरन और दर्द भरा स्पन्दन ।
चुहचुही चिड़िया ने भोर होने की सूचना चुहचुहाते बोलों से दिया तो बाँसुरी और घुंघुरुओं की ध्वनि विलीन हो गई । ब्रह्मबेला का वह पौर्णमासी का चन्द्र था । सारी प्रकृति रेशमी शाल ओढ़कर सोइ हुई थीं --- मासूम बच्चे की तरह या कामनारहित परमहंस की भाँती ।
सूर्योदय हो गया । हिम कणों से भीगी हुई प्रकृति अभ्यंग स्नान किए हुए किसी सुहागिन नवयौवन - सी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानों प्रकृति वधू फूलों का चौक पूर कर देव - पूजन की तैयारी कर रही है । सूर्य क्षितिज पर युग आया था कुहासा विलील हो चुका था ।
मैं प्रातः के प्रकाश में झील का किनारा छोड़कर मार्ग ढूंढ रहा था । अचानक मुझे सैकड़ो नर - नारियों के शव बिखरे हुए दिखाई पड़े । मैं भयभीत हो उठा । सारी हेकड़ी हवा हो गई । सारी विरक्ति, अनुरक्ति वहीं छोड़कर मैं भाग चला । भाग्य या भय ने मुझे राह दिखाई ।
१ हिमालय की उस झील का सौन्दर्य, उसका रहस्य और वहाँ बिखरे हुए शव मुझे निरन्तर सत्ता रहे थे । २३ वर्ष बाद सन् १९५८ ई, में उत्तर प्रदेश राज्य के वन मन्त्री श्री जगमोहन सिंह नेगी ने समाचार पत्रों में उस झील और नर कंकाल का वर्णन करते हुए उसे रूप कुंड बताया, किन्तु बाँसुरी और घुंघुरुओं की ध्वनि की कोई चर्चा नहीं की थी।
हिमाच्छादित पथ पर हिम मानव बनकर मैं भाग रहा था । मुझ भय ग्रस्त को भागते हुए देखकर कस्तूरी मृग, भूरे भालू पहले चकित दृष्टि से मुझे देखते फिर वह भी पलायन धर्म अपना कर जिधर उनका मुँह था उधर ही भागते थे । मैं गिरता, पड़ता, चढ़ता, उतरता कब तक भागता रहा - इसका तो कुछ होश नहीं था । मेरा भय मुझे पथ दिखा रहा था उस समय वही पथ बन्धु था मेरा । दोपहर ढलते - ढलते मैं लस्त पस्त होकर एक मैदान में पहुँचकर गिर पड़ा । शाम को भेड़ों के चरवाहों ने मुझे उठाया । वह अपने डेरे पर ले गए । मुझे सँभलने में १७ दिन लग गए । उन गड़रियों ने मेरी बड़ी सेवा की । फिर उन्हीं के साथ भेड़ें चराता हुआ मैं ग्वालदम पहुंच गया । ग्वालदम के एक पठारी जंगल में डेरा डाल दिया गया था । तीन दिन बिताने के बाद चौथे दिन जब मैं भेड़ों के पीछे ' हुर्र - हुर्र ' करता उन्हें चरा रहा था , तो स्वामी शान्तानन्द आ गए । मुझे देखकर मुस्कुराते हुए शान्तानन्द बोले -- क्षीर स्वामी, लौट आए ऋचाओं की जन्मभूमि से । मैंने कहा -- क्षीरस्वामी वहाँ लौट कर विपथगामी बन गए हैं, स्वामी जी । देख तो रहे है । यह सुन कर वह बड़ी जोर से हॅसे और आगे बढ़कर उन्होंने मुझे ह्रदय से लगा लिया । आज ही चलना है । मैंने कहा कि मेरी हालत अब पहाड़ चढ़ने उतरने कि नहीं है । क्षत - विक्षत शरीर को किसी प्रकार भेड़ों के सहारे घसीट रहा हूँ ।
जो कुछ पहने, ओढ़े हूँ, वह मेरे लिए दीनानाथ बने गड़रियों के है । उनका मुझ पर जो ऋण है, उसे उनकी भेड़ें चराकर उतारने के बाद कहीं जा सकूँगा । यह सुन कर स्वामी जी गड़रियों के दल के मुखिया से भेट कर उन्हें तीन सौ रुपया दिए, फिट लौटकर वह कहीं चले गये एक दिन बाद मेरे पहनने ले लिए कपडे और आवश्यक सामग्री लेकर आए । एक दिन उन्होंने भी गड़रियों के बीच रहकर मेरा उपचार जड़ी - बूटियों से करके मुझे सशक्त और चैतन्य बना दिया । फिर हम उधर से ही तीन दिन की यात्रा करके कर्ण प्रयाग पहुंच गए ।
हिमालय मेरी बाहों में
पंडित देवदत्त शास्त्री"
2)-**मेघदूत की अलका***
इलाहाबाद में गंगा के किनारे शिवकुटी एक सुंदर स्थान है यहीं पर नेपाल के राणा खानदान के वे लोग स्थाई रूप से रहते हैं जिनके पूर्वजों को नेपाल से निकाल दिया गया था शिवकुटी में रहते हुए इस खानदान ने अपनी वंश परंपरा और उपाधि नहीं छोड़ी यहां भी राजा साहब कहलाते रहें और उनकी रईसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
राणा साहब गीता के बड़े भक्त थे ,इतने भक्त की 5 वर्ष के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको गीता कंठस्थ थी रानी साहिबा, राजकुमारियां ,और राजकुमार नित्य शाम को हंडिया बाबा के यहां सत्संग करने आते थे घूमते घूमते मैं भी शिवकुटी पहुंच गया और हडिया बाबा के यहां ही अपनी कमरी बिछा दी, मामूली-सी छोटी कुटी थी किंतु उसके अंदर एक विशाल गुफा थी बड़ी साफ-सुथरी जाड़े में मेरे लिए गुफा जिरह बख्तर बन गई। हंडिया बाबा के लिए मैं एक समस्या बन गया था इसलिए कि वह तो मधु करी भिक्षा करते थे मेरे लिए आटा दाल का प्रबंध पहले दिन तो कर दिया किंतु जब मैंने बताया कि मुझसे खाना बनाते नहीं बनता तब यह बड़े संकोच में पड़ गए मुझे क्या खिलाए?बिना मुझे खिलाए खुद खा लेना उचित नहीं था! मैंने उनकी इस दुविधा को अनजाने में ही हल कर दिया था ,उनकी भिछा से भिक्षा मांग कर हडिया बाबा पढ़े लिखे तो नहीं थे किंतु शील सदाचार संपन्न तपस्वी थे, राणा खानदान उनके सामने गीता, योगवाशिष्ठ के श्लोकों की सेना जमा कर देता और हनिया बाबा सीधी-सादी भाषा में व्यावहारिक दृष्टांतो से उनकी जिज्ञासा शांत किया करते थे। जिस दिन मैं पहुंचा था उसी दिन शाम को राजपरिवार सत्संग के लिए हंडिया बाबा के पास आया मुझे नवागंतुक जानकर मेरा परिचय पूछा गया, परिणाम यह हुआ कि बोझा बलइया मैं हंडिया बाबा के सिर से उतरकर राणा साहब पर सवार हो गया।
राणा साहब के यहां कुछ दिन रहने के बाद उनके साथ नेपाल गया,वहां इस समय के कमांडर-इन-चीफ मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा(बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री) से परिचय हुआ। राणा साहब कालिदास के काव्यों में अत्यधिक अनुराग रखते थे।मेघदूत की कल्पना की उन्होंने भूरि भूरि प्रशंसा की मैंने कहा श्रीमान् मेघदूत का विरही यक्ष काल्पनिक नहीं है ,पौराणिक है। उसके शाप की कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण के एकादश खंड में लिखी है। उसी को आधार मानकर कवि की कल्पना मुखरित हुई है, यक्ष ने जहां जहां मेघ को भेजा है वह भारतीय भूगोल के विख्यात स्थान हैं, उनके वर्णन भी यथार्थ हैं।
मेघदूत काल्पनिक नहीं यथार्थवादी काव्य है, मेरी यह बात सुनकर राणा साहब ने मुझे मेघदूत का अध्ययन इस ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें भौगोलिक तथ्य और कल्पना से भीगी हुई कथा कि यथार्थता स्पष्ट हो।
मैंने कहा लिखने से पहले उन स्थानों को देखना आवश्यक है जिनका वर्णन मेघदूत में है।
कालिदासकालीन इन स्थानों की स्थिति से आज की उनकी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन देना आवश्यक है।
"आप जा सकेंगे'-राणा जी ने पूछा।
' मुझे एतराज नहीं यदि आपका सहयोग मिले ।'
मेरे यह कहने की देर थी कि राणा जी मुझसे भी ज्यादा सनकी साबित हुए।भरपूर आर्थिक सहायता देकर उन्होंने मुझे विदा किया।मैंने कंबल लोटा सोटा उठाया और नेपाल से प्रस्थान किया ,पहले चित्रकूट के आसपास भ्रमण किया पर्वतों के नाम मैदानों के नाम के आधार पर आधुनिक संख्याओं से मेल बैठाते हुए भेलसा, उज्जैन पहुंचा । वहां से लौटकर रामटेक भी गया, क्योंकि कुछ लोग रामटेक को ही रामगिरी मानते हैं फिर उज्जैन, मंदसौर होता हुआ चंबल नदी के बीहड़ों में मैंने प्रवेश किया ,कभी ट्रेन से कभी पैदल घूमता हुआ, मैं कनखल तक पहुंच कर रुक गया, अब मुझे कुबेर की अलकापुरी देखनी थी! अलका कहां है? वह सरोवर कहां है? जहां यक्ष कमलों की रखवाली करता था। पुराणों के भूगोल से अनुश्रुतियों से कहीं अलका माणा गांव के पश्चिम सतोपथ के आसपास ठहरती ,कहीं बद्रीनाथ धाम के पास और कहीं कैलाश मानसरोवर के पास ।
प्रबुद्ध पर्यटकों, पंडो ,और पुरातत्त्ववेत्ता एवं संतों महात्माओं सभी से अलका का परिचय पूछा ।जितने मुंह उतनी ही बातें सुनी कुछ फैसला न कर पाया जितना देख चुका था उसका विवरण राणा साहब को नेपाल भेजकर मैं शांत हो गया ।
2 साल बाद घूमता- घूमता कश्मीर गया नेपाल की भांति कश्मीर का राजकीय पुस्तकालय भी प्राचीन ग्रंथों का अद्भुत संग्रहालय हैं !उसके अध्यक्ष उन दिनों पंडित हरिदत्त शास्त्री थे ,वह वयोवृद्ध होने के साथ ही महान विद्वान और आजकल की भाषा में प्रबुद्ध रिसर्च स्कॉलर थे।मैंने उनके पास जाता, एक दिन बात बात में मेघदूत की अलका का स्मरण हो आया ,मैंने उनसे पूछा अलका कहां है?और वह सरोवर कहां है? शास्त्री जी ने बताया कि आधुनिक चित्राल पर्वत की श्रंखला है, वही कुबेर का बगीचा चैत्ररथ था ,चैत्ररथ ही बिगड़ कर चितराल बन गया है यह सुनकर मेरी उत्सुकता जागी और मैं चित्राल के उस स्थान में जाने के लिए व्याकुल हो गया जहां पर यक्ष ने कमल पुष्पों की रखवाली करते हुए असावधानी की और प्रिया विरह का स्थान पाकर वह स्वर्ग से मृत्युलोक में भेज दिया गया। शास्त्री जी ने वैदिक, पौराणिक ,भूगोल के आधार पर मुझे समझाया कि सर्वप्रथम सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से विश्व का सर्वेक्षण किया गया, तो ब्रह्मा ने अखिल विश्व को देव त्रिलोकी और असुर त्रिलोकी इन दो भागों में बांट दिया, देव त्रिलोकी के अंतर्गत स्वर्ग लोक ,अंतरिक्ष लोक, और मनुष्य लोक तीन विभाग किए गए ।शर्पणावत( शिवालिक पर्वत श्रेणियां) पर्वत से 90 अंश उत्तर अंतरिक्ष लोक था ,उससे उत्तर प्राग्मेरु(पामीर का पठार) से लेकर साइबेरिया तक स्वर्ग लोक था ,और दक्षिण अंतरिक्ष लोक से दक्षिण का भूभाग मनुष्य लोक था! कुबेर अंतरिक्ष लोक का राजा था, इस लोक में यक्ष, किन्नर ,गंधर्व पिसाची, गुह्क,नाग, पन्नग आदि योनियों के लोग रहते थे। चैत्ररथ कुबेर का उद्यान था ,इस उद्यान भूमि के अधिकारी कुबेर का पुत्र नलकुबेर था, कश्मीर से पश्चिम उत्तर कक्का (केकय) की द्रोणी से ईशान कोण की ओर (कुछ अक्षांशभी बताया था जो अब याद नहीं) चितराल का जो कच्छा शिखर है उसी के ऊपर वह सरोवर है जहां यक्ष कमल पुष्पों की रखवाली किया करता था।
मेघदूत के अध्ययन अनुवाद का संकल्प उसके परिकल्पना भूलकर मैं चितराल देखने के लिए व्यग्र हो उठा मेरी पैदाइशी यायावरी वृद्धि मचलने लगी शास्त्री जी ने मेरी इस उत्कंठा और जिज्ञासा को दुस्साहस और खतरनाक कदम कह कर मुझे रोकना चाहा, किंतु मैंने निवेदन किया कि महाराज मैं तो लड़कपन का यायावर(आवारा), मेरे आगे नाथ न पीछे पगहा बना है मुझे ठीक से रास्ता समझा दें ।बहुत अनुनय विनय करने के बाद शास्त्री जी ने एक नक्शा तैयार किया फिर भी उन्होंने समझाया कि पग पग पर अकाल मृत्यु का भय है मेरे दुस्साहस भरे आग्रह और अनुनय विनय से द्रवित हो गए और तत्कालीन कश्मीर नरेश महाराजा हरि सिंह के मेरे पागलपन की बात कही तो राज महल में मेरा बुलावा हुआ ,पहले तो महाराज ने मुझे शेखचिल्ली समझा पर बाद में शायद उन्हें दया आई या जो भी बात हो उन्होंने चितराल यात्रा के सभी साधन सुविधाएं स्टेट की ओर से प्रदान की कश्मीर नरेश के इस अप्रत्याशित अनुग्रह से मेरे संकल्प को बल मिला मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं कुबेर का उद्यान और वह सरोवर जरूर देखूंगा जहां यशकमल पुष्पों की रखवाली किया करता था, गाइड कुली और घोड़े मिलाकर हम 22 प्राणियों का काफिला रवाना हुआ शास्त्री जी के निर्देशन पर स्टेट के नक्शा नवीस ने हमारा जो पद चित्र तैयार किया था वह मेरी समझ में बहुत कम आया, इस मामले में मेरा गाइड मुझसे कहीं अधिक योग्य था।
हम पहाड़ों नदियों जंगलों को पार करते हुए कक्का पहुंचे प्राचीन केकय ही आजकल कक्का कहलाता है।बीहड़ जंगल उत्तुंग पर्वत शिखरों में यह वन्य प्रदेश आज भी संस्कृति सभ्यता का स्पर्श न कर सका यह वही प्रदेश है जहां अश्वपति ब्रह्म विद्या के अद्वितीय ज्ञानी केकय राजा राज्य करते थे ,जिनके यहां बड़े-बड़े ऋषि मुनि हाथ में कुशमोटक लेकर ब्रह्म विद्या सीखने आया करते थे ,यहीं पर अनिन्द्या सुंदरी के कैकेयी पैदा हुई थी,किंतु मैंने जब कक्का को देखा तो वह एक शासित प्रदेश निर्जन स्थान मुझे दिखाई पड़ा अश्वपति और कैकेई के वंशज नग्न अर्धनग्न अवस्था में मानव होकर भी वन्य जीवन व्यतीत करते हैं ।वहां अभी चकमक पत्थर से आग बनाई जाती है ,पेड़ों की छाल और पत्तियां अथवा जंगली जानवरों की खाल ही उनका परिधान है ,कच्चा मांस ,फल ,फूल कंद ही उनका भोजन है, हमारा गाइड भी वहां पहुंचकर फेल हो गया ,वह उनकी भाषा से तो सर्वथा अपरिचित ही रहा साथ ही उनके पाषाण युगीन अस्त्र शस्त्रों को देख कर उसे प्राण संकट का अनुभव हुआ।उन वनवासियों के लिए धन दौलत का कोई महत्व नहीं, शिकार और नृत्य यही दो उनकी जिंदगी के लक्ष्य थे, उन्हें खाद्य सामग्रियां देकर गाइड ने उनका अनुग्रह प्राप्त किया सौभाग्य था कि वे चितराल से परिचित थे कुछ भाषा से कुछ इशारों से यह ज्ञात हो सका कि चितराल वहां से उत्तर-पश्चिम है किंतु चितराल के जिस शिखर पर हमें जाना था उसका कुछ पता न चल सका नक्शे के आधार पर रामभज कर हम चल तो पड़े किंतु हमारे सभी साथी शिथिल और निराश से जान पड़ते थे उन्हें कोई उत्सुकता नहीं थी पेट और गुलामी उन्हें मजबूर बनाए हुए हुए था हमें इन पर्वतों से बहुत जूझना पड़ा कहीं वनस्पति कहीं कहीं भयंकर बीहड़ घाटियां कहीं उतावली नदियां पग पग पर जंगली जानवरों से मुठभेड़ और सबसे अधिक पहाड़ी अजगर उनका खतरा हमारे लिए प्राण गवा बन रहा था परमहंस की भांति पड़े हुए भयंकर अजगर उनके ऊपर चढ़कर हमें कई बार चलना पड़ा एक दिन हम लोग एक पर्वत के कट प्रदेश में पड़ाव डाल दिए विश्राम कर रहे थे आज जलाकर चाय बनाने की तैयारी हो रही थी जमीन कुछ ऊंची थी उसी पर हम लोग बैठे हुए थे चाय बन गए सब लोग पी रहे थे और आग जल रही थी कि सहसा हमारे नीचे की धरती हिलती हुई थी जान पड़ी हम सब हिलने लगी ऐसा मालूम हुआ कि भूकंप आ गया है हम लोग घबराकर उठ खड़े हुए जमीन हिलती रही थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि अजगर महाराज करवटें बदल कर झाड़ पहुंचकर प्रकट हो गए पता नहीं कब से वह सो रहे थे उन पर मिट्टी चल गई थी आग की गर्मी से उनकी सर्दी दूर हुई और वे उठे जगने के बाद उनकी भूख भी जाती है और वे अपना विशाल मुंह खोलकर जब हवा खींचते हैं तो 10 20 गज की दूरी पर जो भी जीव जंतु सामने रहता है खींचकर उनके पेट में समा जाता है इस भय से हम लोग वहां से भाग खड़े हुए हमारे गाइड ने अजगर सर्पों से संबंधित बड़ी रोचक और दर्दनाक कहानियां सुनाइए किस तरह गाय भैंस बकरी मनुष्य उनके पेट में समा जाते हैं सुनकर रोमांच हो आया वहां से आगे बढ़ने पर सुनसान निर्जन घाटी मिली उस घाटी में एक शिव मंदिर का पुराना खंडहर मिला उसके स्थापत्य शिल्प को समझने में मैं सर्वथा असमर्थ रहा वह ना तो गुप्त काल का शिल्प था और उसके बाद का इस खंडहर की शिव प्रतिमा संभवतः कसौटी पत्थर की ऊंचाई में इतनी कि सिर पर जल छोड़ने के लिए सी डी लगानी पड़ेगी इतनी किसी के भुज पास में ना सके हम वहीं पर डाल दिया 3 दिन तक पढ़े रहे इस दरमियान हमारे साथियों ने मनोरंजन मनोरंजन में एक अद्भुत रहस्य खोज निकाला प्रातः काल उस शिवलिंग को कोई भी व्यक्ति अखबार में भर सकता था किंतु दोपहर के बाद जब शिवलिंग को दोनों हाथों से भरा जाता तो दो बेटे का फैसला रहता था ऐसा क्यों होता था यह रहस्य अज्ञात ही रहा हमें 2 दिन रहते हुए वहां हो गए थे हमारा गाइड पथ की खोज में व्याकुल था दिशा बोधक यंत्र न होने से हम बिग मूर्ति लक्ष्य का कुछ अता पता न मिलने से चलना भी उचित नहीं था साथ ही खाद्य सामग्री को देखते हुए यात्रा दिवस का निश्चय रखना भी आवश्यक था इसी उधेड़बुन में हम पढ़े थे कि कुछ फिर अंदर अर्धनग्न जातियों का एक दल का की ओर जाते हुए उधर से गुजरात हमारे गाइड ने उनसे बात की क्या बात की या तो समझ में नहीं आया किंतु वह मुंह लटकाए हुए लौटा पूछने पर बताया की अनुमान से चितराल का वह शिखर जहां हमें जाना है यहां से 15 दिन का रास्ता है पग-पग पर खतरा है नदियों के अलावा हिममानव का खतरा सर्वाधिक है मुझे ऐसा आभास हुआ कि गाइड मुझे धोखा दे रहा है यह जाना नहीं चाहता है और मेरे ही मुंह से नहीं करा कर लौटना चाहता है लौटकर महाराजा हरि सिंह को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं चिंतित हो उठा एक दिन और ठहर कर चलने के लिए तैयारी की तो शायद गाइड का इशारा पाकर कुलियों ने असहयोग कर दिया ना जाने के लिए तैयार नहीं थी मैं ना तो अकेले जा सकता था और ना लौटना ही चाहता था मेरी हालत सांप छछूंदर की सी हो रही थी साथ ही कुबेर का उद्यान देखने की अतिरिक्त परिभाषा थी गाइड के साथ सभी साथियों ने जब आगे चलने से इनकार किया तो मैंने कुछ आवश्यक सामग्री उनसे उतनी ही जितनी लेकर मैं दुर्गम पर्वतों पर चल और चढ़ सकता था इसके बाद उन्हें लौट जाने की अनुमति देकर जब मैं चलने लगा तो उनमें से एक व्यक्ति को न जाने क्या सूझी कि उसने अपने साथियों के सामने यह रखा कि 1 सप्ताह तक सब यहीं रुके हैं और वह मुझे साथ लेकर चितराल जाएगा कदाचित 1 सप्ताह में हम ना लौट सके तुम्हें लोग लौट जाएं थोड़े से जद्दोजहद के बाद यह प्रस्ताव सब ने स्वीकार कर लिया और हम दोनों आगे बढ़ चले 6 घंटा चलने के बाद उसने नक्शा खोला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और नक्शे पर उंगली फिरता हुआ वह बोला कि हमें जाना इधर चाहिए था और हम इधर भटक गए वही हमने उस दिन पड़ाव डाल दिया और आपस में मार्ग संबंधी विचार विनिमय करते रहे दूसरे दिन हमें एक ऐसा पहाड़ मिला जिसे पार करना हमारे बस की बात न थी पहाड़ों पर चढ़ते उतरते हमारा जिओ गया था हम जब किसी पर्वत शिखर पर चढ़ते तो यह आशा बनती कि इसके बाद मैदान मिलेगा किंतु उस से भी ऊंचा दूसरी ओर पर्वत शिखर खड़ा मिलता पहाड़ों से अधिक कष्टदायक पहाड़ी नदियां हुआ करती हैं चौड़ाई जरा सी किंतु प्रवाह में आग तूफान की तेजी और जरा सा चुके की ऐसी ही एक नदी ने हमारा पीछा किया कहीं से भी हम चलें घूम फिर कर वह घेर कर खड़ी हो जाती थी निराश होकर हमें उसका ही आंचल थाम लिया मौत से लड़ते हुए हम नदी के किनारे 3 दिन तक चलते रहे चौथे दिन उस नदी ने एक ऐसे पहाड़ के नीचे हमें लाकर खड़ा किया जो विराट दानों की तरह आना था और नदी उसकी छाती चीरकर उसमें प्रविष्ट हो गई थी ऐसा मालूम पड़ता था कि नदी उसी पहाड़ से ही निकली थी समूचा पहाड़ एक भयंकर दर्रा था हम लोगों ने भाई और चढ़कर एक छोटे से शिखर को पार किया तो हमें एक बहुत ही हरी-भरी सुंदर घाटी मिली एक और पर्वतमाला और दूसरी ओर हरा भरा मैदान बहुत रमणीक स्थान था वह अन्य वही दो 1 दिन ठहर कर मन मस्तिष्क और शरीर की थकावट मिटाने का इरादा किया कुछ दूर चलकर एक सरोवर मिला पशु पक्षियों के दर्शन हुए हमने उससे कुछ हटकर अपना रेन बसेरा बनाया प्रभात काल में हम उठे धूप निकल चुके थे हमने देखा कि एक आदमी सरोवर से पानी लेकर जा रहा है हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों आदमी तोड़कर उसके पीछे पीछे हो लिए पर्वत के अंतराल में बनी एक गुफा में वह प्रविष्ट हो गया तो हम भी उसके पीछे-पीछे वहां चले गए हमने देखा कि वह कोई जंगली नहीं बल्कि महात्मा है मैंने उनके चरण छूने का प्रयत्न किया तो वह उछल पड़े और मुस्कुराते हुए बोले तुम लोग यहां कैसे मैंने सारी कष्ट कथा और अपना बचपन उनसे बताया तो उन्होंने मुस्कुरा कर फिर कहा वह तो यही है सामने दिखाई पड़ रहा है यही है सुनकर मैं संज्ञा सुनीसा हो गया मुझे ऐसे भान हुआ जैसे जीवन की सर्वोत्तम निधि मिल गई हो बेशक मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण था महात्मा ने हमें एक दिन रुक कर दूसरे दिन वहां ले चलने का वायदा किया उन्होंने बताया कि अनजाने रास्ता पाना कठिन है पहुंचना असंभव है उन्होंने हमें कुछ कंदमूल खाने को दिए जिन्हें हम कच्ची शकरकंद की तरह जब आ गए दूसरे दिन हम दोनों महात्मा जी के साथ चल पड़े 4 घंटे बाद हम उस शिखर के ऊपर पहुंचे कछुए की पीठ की तरह पढ़ाओ का आशीर्वाद था असम की जड़ी बूटियां और वनस्पतियां की पहाड़ के शिखर पर चढ़ते हुए हम मैदान का अनुभव कर रहे थे महात्मा जी ने बताया कि यहां एक सरोवर है यहां मनुष्य के चरण शायद बहुत कम पढ़े हो यह लोग यही है यहां आ जाता है तो उठा ले जाती हैं इतना मत लाकर महात्मा जी ने कहा अच्छा घूम फिर कर तुम लोग उतरा ना हम चलते हैं उनका कथन इतना प्रभावशाली था कि हम उन्हें रुकने या अपने साथ ले चलने के लिए कुछ ना कह सके वे चले गए हम दोनों पहाड़ की पीठ पर घूमते हुए उस जगह पहुंचे जहां विशाल सरोवर लहरा रहा था जीवन में पहली बार नीलकमल वही देखे सरोवर कमल पुष्पों और चित्र विचित्र पक्षियों से आकर्षण था हम उसके किनारे मंत्रमुग्ध से बैठे हुए थे समस्त पर्वत शिखर एक नैसर्गिक उद्यान बना हुआ था तरह तरह के फल फूल लता विटप उसकी गोद में भी हंस रहे थे यह कुबेर का उद्यान हो या ना हो वह सरोवर वही हो या ना हो इसके कमल पुष्पों की रखवाली मेघदूत का अक्स करता था कुबेर की अलका वही थी या नहीं इस विवाद से मैं रहित हो गया मैं एक अत्यंत आनंद सागर में डूबा हुआ था मेरे हृदय में एक अद्भुत शांति छाई हुई थी घंटों सरोवर को निहारता रहा इतने में शाम हो गई मेरा साथी मुझसे भी अधिक लापरवाह निकला उसने एक शब्द भी मुझसे ना कहा चुपचाप वह भी बैठा रहा अब रात में पहाड़ कैसे उतरेंगे मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि आज की रात यही बिताई दे तब मुझे एक चिड़ियों के उठा ले जाने वाली स्वामी जी की बात याद आई मैंने कहा जिंदगी में एक श्रेणियों के भी दर्शन हो जाएंगे उठा ले गई उनके घर द्वार रहन-सहन का भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे बचेंगे तो जीवन का एक राशि प्राप्त कर लौटेंगे नहीं बचेंगे तो भी सदैव स्वर्ग प्राप्त करेंगे चांदनी चिपक गई सारा पर्वत पृष्ठ सुगंधित से महा महा रहा था हमारी भूख प्यास हर गई थी केवल जिज्ञासा प्रबल थी हम इधर उधर घूम कर बंसी का अश्वर्य देख रहे थे
चांदनी मुस्कुरा रही थी रात भीगने लगी थी कि हमें एक स्थान पर सैकड़ों हजारों घुंघरू तालसर से बचते हुए सुनाई पड़े हम दोनों उस जगह गए तो वहां से हट कर दूसरी जगह ध्वनि सुनाई पड़ने लगी जहां हम जाते वहीं से हटकर दूसरी जगह नृत्य संगीत का वह मधुर गुंजन सुनाई पड़ता हम विक्षिप्त से हो रहे थे सारी रात उसी तरह घूमते गुनोपुर धन सुनते रहे दिखाई कुछ लफड़ा सवेरा हो गया कमल पुष्प खिल कर हंसने लगे थे सरोवर के जल का मार्जन आचमन कर हम जिस रास्ते से आए थे उसी से नीचे उतरकर महात्मा जी के पास आए उनसे रात की घटना बताई तो वह बोले नहीं मुस्कुराते रहे तीन दिन तक हम वही विश्राम करते रहे लौटने के लिए हिम्मत छूट गई थी कोई साधन नहीं पथ नहीं निश्चय था कि अब लौट न सकेंगे हमारी इस निराशा और वेदना को समझकर स्वामी जी ने हमें बताया कि जिस नदी का किनारा पकड़कर तुम आए हो उसी के किनारे किनारे चले जाओ अब तुम्हें पर्वत की एक बड़ी विशाल धोनी मिले तब नदी को छोड़कर पूर्व की ओर सीधे चलते जाना उधर ही गिरगिट पहुंचकर कश्मीर पहुंच जाओगे चलते समय महात्मा जी ने हमें किसी वृक्ष की एक हरी हटाने दी और कहा कि अंधेरे में इसे हाथ में रखना यह प्रकाश देगी वह कहानी कभी सुखी नहीं लगभग डेढ़ महीना तक हमें प्रकाश देती रही अंधेरे में उसे प्रकाश फूटा था मानो हम दीपक लिए हुए हैं रास्ता भी ऐसा मिला कि खाने-पीने की कमी नहीं हुई सुंदर से सुंदर फल नित्य मिलते रहे 20 दिन बाद हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां हमें गिरफ्तार कर बड़े आराम से गिरगिट ले जाया गया वहां हम 10 दिन तक कैद रहे फिर ब्रिटिश पोलिटिकल एजेंट के सामने पेश किए गए हमसे अंग्रेज अफसरों ने तरह-तरह से सवालात किए हमने जो सही बात ही बतला दिए तब वायरलेस से श्रीनगर से पूछा गया इत्मीनान कर लेने के बाद कश्मीर राज्य के अनुरोध पर हमें गिरगिट के पोलिटिकल एजेंट ने यात्रा के साधन और गाइड देकर श्रीनगर पहुंचा दिया महाराज हरि सिंह ने को अपनी यात्रा का पूरा विवरण जब मैंने दिया तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा अंत में मैंने वह कहानी भी उन्हें भेंट कर दी जो हमें अंधेरे में प्रकाश दिया करती थी।
पं देवदत्त शास्त्री
स्मृति के हस्ताक्षर
3)-पण्डित देवदत्त शास्त्री जी ने निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया-
१-अभीष्ट कार्य करने से लाभ होगा या नहीं?
२-युद्ध में, शास्त्रार्थ में, विवाद में, द्यूतक्रीडा में, विजय होगी या नहीं?
३-रोगी रोगमुक्त होगा या नहीं?
४-नौकरी अथवा जीविका का व्यवसाय मिलेगा या नहीं?
५-अनुष्ठित साधना या तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धि पूर्ण होगी या नहीं?
६-नष्ट धन,अपहृत सम्पत्ति,चोरी गया धन, अपहृत या भागा हुआ, प्राणी प्राप्त होगा या नहीं।
७-किसी भी प्रकार की परीक्षा में सफलता मिलेगी या नहीं?
८-वर को वधू या कन्या को योग्य वर मिलेगा या नहीं?
९-उत्तम वर्षा, अच्छी फसल होगी या नहीं?
१०-पुत्र की प्राप्ति होगी या नहींं?
भले ही अथर्ववेदीय प्रश्न ज्योतिष् के अन्तर्गत पण्डित देवदत्त शास्त्री जी ने इन प्रश्नों का उल्लेख किया है, किंतु यही प्रश्न सही मायने में आज की सार्वभौमिक समस्यायों का संदर्शन है।
पण्डित देवदत्त शास्त्री जी ने इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने ग्रंथ"अथर्ववेदीय तंत्र विज्ञान" में दिया है, जिससे आधुनिक दौर में जब अब तक के वैज्ञानिक अनुसंधान कोरोना आदि जैसी आपदाओं, महामारियों के समक्ष विफल हो रहे हैं, तो आवश्यकता है, वैदिक, आयुर्वेदिक इत्यादि भारतीय विज्ञान की, जो निश्चित रूप से सभी प्रकार की समस्यायों का समाधान करता है, क्योंकि वैदिक और भारतीय विद्वानों ने समस्त समस्यायों को दुखत्रय में निर्धारित कर उनके निवारणार्थ अपना अभिमत व्यक्त किया है।
Copyright © 2025 SSAARC. All Rights Reserved.
Design by SoftFixer.com